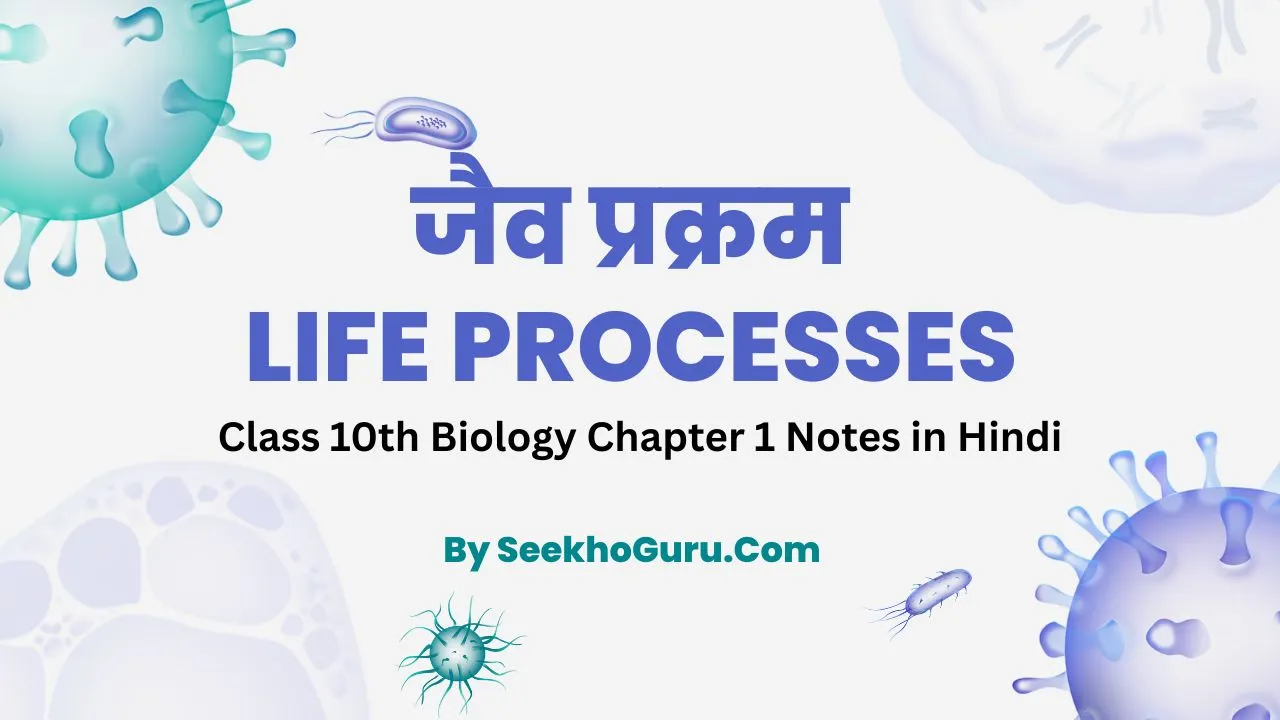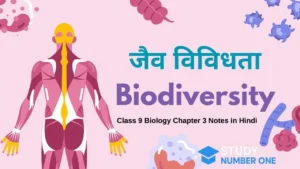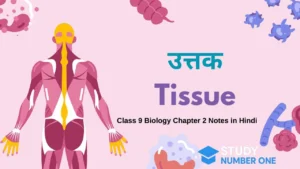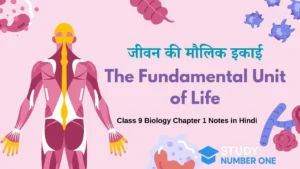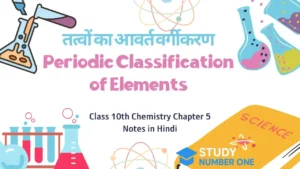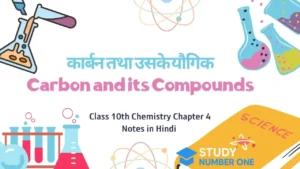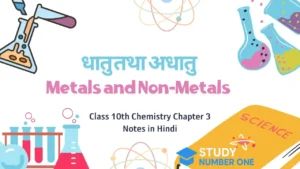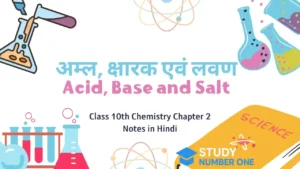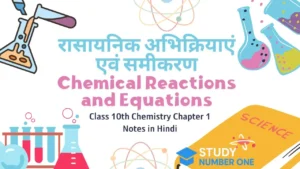Class 10th Biology Chapter 1 Notes in Hindi – जैव प्रक्रम : पोषण के इस पोस्ट में हम आपको पूरी तरह से NCERT syllabus आधारित, सरल और स्पष्ट भाषा में तैयार पोषण (Nutrition) टॉपिक के सम्पूर्ण नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं।
यह नोट्स विशेष रूप से Bihar Board, CBSE, और अन्य राज्यों के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें शामिल है — पोषण के प्रकार, मानव पाचन तंत्र, पाचन क्रियाएँ, अंगों का कार्य, आवश्यक एंजाइम्स, चार्ट और आवश्यक चित्रों के साथ सरल व्याख्या।
अगर आप Class 10th Biology Chapter 1: Life Processes के अंतर्गत Nutrition विषय को आसानी से समझना चाहते हैं, तो यह फ्री नोट्स और PDF डाउनलोड आपके लिए परफेक्ट हैं।
👉 अभी डाउनलोड करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बनाएं आसान।
Class 10th Biology Chapter 1 Notes in Hindi
जैव प्रक्रम (Life Processes)
शरीर की वे सभी जैविक क्रियाएं जो जीवधारियों को टूट-फूट, क्षय, विकृति तथा बाहरी वातावरण के हानिकारक प्रभावों से बचाकर उनके जीवन के अनुरक्षण (maintenance) में सहायक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं।
ये प्रक्रियाएं जीव के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं और इनका निरंतर संचालन ही जीवन का परिचायक होता है। प्रमुख जैव प्रक्रमों में पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन सम्मिलित हैं।

जैव प्रक्रम के प्रकार
- पोषण (Nutrition) – वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा उत्पन्न करने, शरीर की वृद्धि, निर्माण, मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग करता है, पोषण कहलाती है।
- श्वसन (Respiration) – वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है।
- परिवहन (Transportation) – शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक तत्व, गैसें एवं अपशिष्ट पदार्थ पहुँचाने की क्रिया।
- उत्सर्जन (Excretion) – शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया।
- प्रजनन (Reproduction) – नए जीवों का निर्माण करने की प्रक्रिया।
- वृद्धि (Growth) – शरीर के आकार, ऊँचाई एवं भार में वृद्धि होना।
1. पोषण (Nutrition)
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा उत्पन्न करने, शरीर की वृद्धि, निर्माण, मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग करता है, पोषण कहलाती है
पोषण के प्रकार
- स्वपोषण (Autotrophic Nutrition) – वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे – हरे पौधे। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं।
- परपोषण (Heterotrophic Nutrition) – वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे – मनुष्य, पशु, अमीबा आदि।
परपोषण के प्रकार
- मृतजीवी परपोषण (Saprophytic Nutrition) – वे जीव जो मृत एवं सड़े-गले जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे – कवक, फफूंदी, कुकुरमुत्ता आदि।
- परजीवी परपोषण (Parasitic Nutrition) – वे जीव जो किसी अन्य जीव (होस्ट) के शरीर में या शरीर पर रहते हुए उससे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे – फीताकृमि, प्लाज्मोडियम (जो मलेरिया फैलाता है)।
- प्राणीसम्मोज परपोषण (Holozoic Nutrition) – वे जीव जो ठोस या तरल भोजन ग्रहण कर उसे शरीर के भीतर पचाते हैं, जैसे – मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा आदि।
- सहजीवी पोषण (Symbiotic Nutrition) – दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन (कवक + शैवाल)।
भोजन (Food)
भोजन वे सभी जैविक पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर अवशोषित होते हैं तथा शरीर की वृद्धि, क्षति की मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन, ऊतकों की संरचना, जनन क्षमता एवं शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होते हैं। भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि उसे स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाए रखता है।
प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)
प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने पर्णहरित (chlorophyll) की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल (H₂O) और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से ग्लूकोज (C₆H₁₂O₆) का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन (O₂) को मुक्त करते हैं।
समीकरण:
6CO₂ + 6H₂O + सूर्य का प्रकाश ⟶ C₆H₁₂O₆ + 6O₂
हरित लवक (Chloroplast)
यह पत्ती में उपस्थित हरे रंग की अंडाकार रचनाएं होती हैं जिनमें हरित वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यही रचना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सम्पन्न करने में सहायक होती है।
रंजक (Pigments)
रंजक वे जैविक अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की विशेष तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल, जो लाल और नीली रोशनी को अवशोषित करता है तथा हरी रोशनी को परावर्तित करता है।
पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं?
पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रंजक लाल एवं नीली तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि हरी रोशनी को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए पौधे हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं।

पर्णहरित के घटक (Components of Chlorophyll)
पर्णहरित (Chlorophyll) वह रंजक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई उपघटकों से मिलकर बना होता है:
- पर्णहरित ए (Chlorophyll-A) → नीला-हरा (Blue-Green) रंग
- पर्णहरित बी (Chlorophyll-B) → पीला-हरा (Yellow-Green) रंग
- जैन्थोफिल (Xanthophyll) → पीला (Yellow) रंग
- कैरोटीन (Carotene) → नारंगी (Orange) रंग
ये सभी रंजक पौधे की पत्तियों में उपस्थित होते हैं और विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्रदान करते हैं।
एंजाइम (Enzymes)
एंजाइम शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जैविक उत्प्रेरक (Biological Catalysts) होते हैं, जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को तेज करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन आदि। ये प्रोटीन से बने होते हैं और हर एंजाइम एक विशेष प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है।
रंध्र (Stomata)
रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो गैसीय विनिमय (CO₂ का ग्रहण एवं O₂ का निष्कासन) और जल वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) में सहायक होते हैं। प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं (Guard Cells) द्वारा घिरा होता है जो इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं।
उपापचय (Metabolism)
कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है:
- उद्विकरण (Anabolism): निर्माण क्रियाएं जैसे – प्रोटीन संश्लेषण।
- अपचयन (Catabolism): अपघटन क्रियाएं जैसे – ग्लूकोज का विघटन।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कैसे? (प्रयोग)
प्रयोग:
जलीय पौधे हाइड्रिला की कुछ टहनियाँ लेकर एक जल से भरे बीकर में रखें। फिर एक कीप को उल्टा करके उसमें डालें ताकि टहनियाँ पूरी तरह ढक जाएँ। कीप के मुँह पर एक जल से भरी नलीदार बोतल (test tube) को उल्टा रख दें। इस व्यवस्था को धूप में रखें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हाइड्रिला की टहनियों से बुलबुले निकल रहे हैं। परीक्षण करने पर यह पुष्टि होती है कि वे बुलबुले ऑक्सीजन गैस के हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है।
अमीबा में पोषण (Nutrition in Amoeba)
अमीबा एक एककोशिकीय जीव है जो प्राणीसम्मोज पोषण करता है। यह अपने आसपास के भोजन को कुटपाद (Pseudopodia) की सहायता से घेरकर एक खाद्य्यानी (Food Vacuole) बनाता है।
- खाद्य्यानी में पाचक एंजाइम प्रवेश कर भोजन को पचाते हैं।
- पचा हुआ भोजन कोशिका में अवशोषित हो जाता है।
- शेष अपच्य अंश को खाद्य्यानी कोशिका की सतह से चिपककर बाहर निकाल देती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कच्ची सामग्री कहाँ से मिलती है?
पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं:
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂): वायुमंडल से, रंध्रों के माध्यम से।
- जल (H₂O): मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित।
- पर्णहरित: पत्तियों के हरित लवक में पाया जाता है।
- सूर्य का प्रकाश: प्रकाश ऊर्जा का स्रोत।
पाचन (Digestion)
पाचन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा) को सरल अणुओं (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड) में तोड़ा जाता है ताकि वे आसानी से अवशोषित होकर कोशिकाओं में उपयोग किए जा सकें।
मनुष्य का पाचन तंत्र (Human Digestive System)

आहार नाल (Alimentary Canal):
मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी नली पाई जाती है जो मुखगुहा से शुरू होकर गुदाद्वार पर समाप्त होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है।
मुखगुहा (Buccal Cavity):
- यह आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है।
- ऊपर और नीचे जबड़े होते हैं।
- दो मांसल ओंठ इसे बंद करते हैं।
- मुखगुहा में दाँत और जीभ उपस्थित होते हैं।
जीभ (Tongue):
- जीभ एक मांसल रचना है जो मुखगुहा के फर्श पर स्थित होती है।
- इसका अगला भाग स्वतंत्र जबकि पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है।
- जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं (Taste Buds) होती हैं जो स्वाद पहचानने में सहायक होती हैं।
दाँत (Teeth):
- दाँत ऊपर और नीचे के जबड़ों में मसूड़ों से जुड़े रहते हैं।
- हर दाँत के तीन भाग होते हैं:
- मूल (Root) – मसूड़े में धंसा भाग।
- ग्रीवा (Neck) – दाँत और मसूड़े के बीच का भाग।
- शिखर (Crown) – जो बाहर दिखाई देता है।
- मूल (Root) – मसूड़े में धंसा भाग।
- दाँत भोजन को चबाने, काटने और पीसने में मदद करते हैं।
दाँत के प्रकार (Types of Teeth)
मनुष्य के मुँह में चार प्रकार के दाँत पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए होते हैं:
| प्रकार | कार्य |
| कर्तनक (Incisors) | भोजन को काटने के लिए |
| भेदक (Canines) | भोजन को फाड़ने के लिए |
| अग्रचवर्णक (Premolars) | भोजन को चबाने व पीसने के लिए |
| चवर्णक (Molars) | भोजन को बारीक पीसने के लिए |
मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है, जिनमें ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में दांत बराबर होते हैं।
इनैमल (Enamel)
दांतों के ऊपर एक कठोर एवं चमकदार सफेद परत पाई जाती है, जिसे इनैमल कहते हैं। यह शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है और दांतों को बाहरी क्षति से बचाती है।
दंत अस्थिक्षय (Tooth Decay)
जब व्यक्ति मीठी वस्तुएँ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाता है और दाँतों की सफाई नहीं करता, तो शक्कर दांतों से चिपक जाती है।
इस शक्कर पर बैक्टीरिया क्रिया करके अम्ल (Acid) बनाते हैं, जो इनैमल पर असर डालकर उसे नरम कर देते हैं। इससे दांत में धीरे-धीरे छिद्र बन जाता है, जिसे दंत अस्थिक्षय या कैविटी कहते हैं।
दंत पलांक (Dental Plaque)
जब भोजन के महीन कण और बैक्टीरिया मिलकर दांतों पर एक परत का निर्माण करते हैं तो उसे दंत पलांक कहते हैं। यदि समय पर हटाया न जाए, तो यह दांतों और मसूड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है।
ग्रसनी (Pharynx)
मुखगुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह दो प्रमुख मार्गों में विभाजित होता है:
- निगल द्वार (Esophageal opening): जो आहारनाल में खुलता है।
- कंठ द्वार (Glottis): जो श्वास नली (Trachea) में खुलता है।
एपिग्लॉटिस (Epiglottis)
कंठ द्वार के ऊपर स्थित एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह भोजन निगलते समय श्वासनली को ढक देती है, जिससे भोजन गलती से फेफड़ों में न चला जाए।
ग्रासनली (Esophagus / Food Pipe)
मुखगुहा में चबाया गया भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रासनली में प्रवेश करता है। यह एक लंबी मांसपेशीय नली होती है।
- इसके दीवारों में लहरों के समान संकुचन और शिथिलन होता है, जिसे क्रमाकुंचन (Peristalsis) कहते हैं।
- यह संकुचन भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है।
अमाशय (Stomach)
अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसकी दीवारें मोटी होती हैं। यह U आकार का होता है और आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है।
- यह ग्रासनली से भोजन ग्रहण करता है और उसे छोटी आंत की ओर भेजता है।
- अमाशय अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे पाचक रस सक्रिय होते हैं।
अमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक रसायन:
- HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल): जीवाणुओं का नाश करता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है।
- पेप्सिन: प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है।
- रेनीन: दूध के प्रोटीन (कैसिन) को पचाता है, विशेष रूप से शिशुओं में।
लार और टायलीन (Saliva & Ptyalin)
- मुखगुहा में स्थित लार ग्रंथियाँ लार उत्पन्न करती हैं जिसमें टायलीन (Ptyalin) नामक एंजाइम पाया जाता है।
- यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज (एक सरल शर्करा) में बदल देता है।
छोटी आंत (Small Intestine)
छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह एक बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है।
- यहाँ भोजन का अंतिम पाचन एवं अवशोषण होता है।
- इसकी आंतरिक सतह पर रसांकुर (Villi) होते हैं जो भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं।
छोटी आंत के भाग:
- ग्रहणी (Duodenum):
- छोटी आंत का पहला भाग
- अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होकर C आकार का होता है
- यहाँ पित्त रस और अग्न्याशय रस मिलते हैं
- छोटी आंत का पहला भाग
- जेजुनम (Jejunum):
- मध्य भाग
- यहाँ पाचन सक्रिय रूप से चलता है
- मध्य भाग
- इलियम (Ileum):
- अंतिम भाग
- इसकी दीवारों पर उंगली जैसी रसांकुर संरचनाएँ होती हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं।
- अंतिम भाग
बड़ी आंत (Large Intestine)
जब भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, तो शेष अवशेष बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं। यह एक लंबी, मोटी नली होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है:
- शेष बचे हुए भोजन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना
- अनपचे अंश को मल के रूप में संग्रहित कर मलोत्सर्जन के लिए तैयार करना
बड़ी आंत के भाग (Parts of Large Intestine):
- सिकम (Caecum):
- छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित एक थैलीनुमा संरचना
- यह शाकाहारी जीवों में सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है
- मनुष्य में इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, इसलिए इसे अवशेषी अंग (Vestigial Organ) कहा जाता है
- छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित एक थैलीनुमा संरचना
- कोलॉन (Colon):
- बड़ी आंत का मध्य भाग
- जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है
- बड़ी आंत का मध्य भाग
- मलाशय (Rectum):
- बड़ी आंत का अंतिम भाग
- इसमें मल संग्रहीत होकर मलोत्सर्जन के लिए तैयार होता है
- बड़ी आंत का अंतिम भाग
एपेंडिक्स (Appendix):
- सिकम के शीर्ष पर एक छोटी अंगुली जैसी रचना होती है जिसे एपेंडिक्स कहते हैं
- इसका सिरा बंद होता है और यह मनुष्य में कोई क्रियात्मक भूमिका नहीं निभाता
- हालांकि शाकाहारी जीवों में यह पाचन में सहायक होता है
भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:
काइम (Chyme):
जब भोजन अमाशय में पहुँचता है तो यह गाढ़े लेई जैसे पदार्थ में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं।
चाइल (Chyle):
जब काइम छोटी आंत में जाकर तरल रूप ले लेता है, तो उसे चाइल कहते हैं।
स्वांगीकरण (Assimilation):
पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद उनका शरीर की कोशिकाओं में उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है।
पित्त (Bile)
- पित्त एक गाढ़ा, हरे रंग का क्षारिय (alkaline) तरल होता है जो यकृत (Liver) द्वारा निर्मित होता है
- इसे पित्ताशय (Gallbladder) में संग्रहीत किया जाता है और भोजन के ग्रहणी में पहुंचने पर इसे वहाँ डाला जाता है
- पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, परंतु इसका पाचन में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है
पित्त के कार्य (Functions of Bile):
- अम्लीय काइम की अम्लता को कम करके उसे क्षारीय बनाता है
- वसा के विखंडन में सहायता करता है
- पायसीकरण (Emulsification): वसा को सूक्ष्म बूँदों में विभाजित करता है जिससे वसायुक्त एंजाइम (lipase) उस पर क्रिया कर सकें
विलाई (Villi):
छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर असंख्य उंगली जैसी रचनाएँ पाई जाती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं।
- ये पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं
- प्रत्येक विलाई के भीतर रक्त वाहिकाएँ एवं लसीका वाहिकाएँ होती हैं जो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं
पाचन ग्रंथियाँ (Digestive Glands)
आहार नाल से जुड़ी वे ग्रंथियाँ जो पाचन में सहायता करती हैं उन्हें पाचन ग्रंथियाँ कहा जाता है।
इनमें प्रमुख हैं:
- लार ग्रंथि (Salivary Gland): मुख में लार उत्पन्न करती है
- यकृत (Liver): पित्त रस का निर्माण करता है
- अग्न्याशय (Pancreas): पाचक एंजाइम युक्त रस का निर्माण करता है
- जठर ग्रंथि (Gastric Gland): अमाशय में जठर रस बनाती है
पाचन ग्रंथियाँ (Digestive Glands)
पाचन ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं:
1. आंतरिक ग्रंथियाँ (Internal Glands):
ये ग्रंथियाँ आहारनाल की दीवारों में पाई जाती हैं और सीधे वहीं से पाचक रस स्रावित करती हैं।
मुख्य उदाहरण:
- स्लेष्मा ग्रंथि (Mucous Gland)
- जठर ग्रंथि (Gastric Gland)
2. बाध्य ग्रंथियाँ (Accessory Glands):
ये ग्रंथियाँ आहारनाल के बाहरी भागों में स्थित होती हैं लेकिन अपनी नलियों द्वारा पाचक रस को आहारनाल में भेजती हैं।
बाध्य ग्रंथियों के प्रकार (Types of Accessory Glands)
(a) लार ग्रंथियाँ (Salivary Glands):
मनुष्य के मुखगुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं:
- पैरोटिड (Parotid)
- सबमैन्डिबुलर (Submandibular)
- सब्लिंगुअल (Sublingual)
इन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलीन, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज में बदलता है। साथ ही ये लार भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी सहायक होती हैं।
(b) यकृत (Liver):
- यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है।
- यह शरीर के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होती है।
- इसका कार्य पित्त (Bile) का निर्माण करना है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है।
(c) अग्न्याशय (Pancreas):
- यह एक पीले रंग की पत्ती जैसी ग्रंथि है, जो अमाशय के नीचे और ग्रहणी से सटा होता है।
- यह एक दोहरा कार्य करता है:
- बाह्य ग्रंथि के रूप में पाचक रस बनाता है।
- अंत: स्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाता है।
पेप्टिक अल्सर (Peptic Ulcer):
जब किसी व्यक्ति के अमाशय की दीवारों पर घाव बन जाते हैं, तो इसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है।
- यह प्रायः उन लोगों में होता है जो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं।
- अम्ल की अधिकता के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।
पायसीकरण (Emulsification):
वह प्रक्रिया जिसमें पित्त के लवणों की सहायता से वसा को छोटे-छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि लिपेज एंजाइम उस पर प्रभावी ढंग से क्रिया कर सके। इसे ही पायसीकरण कहते हैं।
बहिष्करण (Egestion):
बड़ी आंत में शेष बचे अनपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है और फिर उसे मल के रूप में त्याग दिया जाता है।
- इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है।
- यह पाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है।
स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर (Difference Between Autotroph and Heterotroph)
| विशेषता | स्वपोषी (Autotroph) | विषमपोषी (Heterotroph) |
| जीव | केवल हरे पौधे | सभी जानवर, मानव, कवक आदि |
| ऊर्जा स्रोत | सूर्य का प्रकाश | पौधों या अन्य जीवों से |
| CO₂ व जल की आवश्यकता | अनिवार्य | अनिवार्य नहीं |
| पाचन की आवश्यकता | नहीं होती | होती है |
2. श्वसन (Respiration)
वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है।
श्वसन का सामान्य समीकरण:
C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + ऊर्जा
यह एक उपचायक क्रिया (Oxidative Reaction) है।
श्वसन के प्रकार (Types of Respiration):
1. अनॉक्सी श्वसन (Anaerobic Respiration):
- इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।
- ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है।
- परिणामस्वरूप इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
उदाहरण: यीस्ट, हमारी मांसपेशियों में भारी व्यायाम के दौरान।
2. ऑक्सी श्वसन (Aerobic Respiration):
- इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
- परिणामस्वरूप जल, CO₂ और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है।
उदाहरण: सभी उच्च श्रेणी के जीव जैसे मानव, स्तनधारी, पक्षी आदि।
श्वासोच्छवास (Breathing)
मनुष्य में सांस लेने (inhalation) और सांस छोड़ने (exhalation) की प्रक्रिया को श्वासोच्छवास कहते हैं।
- यह एक शारीरिक क्रिया है जो फेफड़ों के माध्यम से होती है।
- इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है।
श्वसन और श्वासोच्छवास में अंतर (Difference between Respiration and Breathing):
| विशेषता | श्वसन (Respiration) | श्वासोच्छवास (Breathing) |
| स्थान | कोशिकाओं के भीतर | कोशिकाओं के बाहर |
| एंजाइम की आवश्यकता | होती है | नहीं होती है |
| प्रक्रिया | जैव रासायनिक | शारीरिक |
| ऊर्जा निर्माण | होता है | नहीं होता |
| गैसों की भूमिका | ऑक्सीकरण के लिए | ऑक्सीजन और CO₂ का आदान-प्रदान |
जीवों में श्वसन के प्रकार (Respiration in Organisms):
1. एककोशिकीय जीवों में श्वसन (Unicellular Respiration):
- अमीबा (Amoeba):
अमीबा में श्वसन कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। इसमें परासरण क्रिया (Osmosis) द्वारा गैसों का आदान-प्रदान होता है।
2. बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन (Multicellular Respiration):
- हाइड्रा (Hydra):
हाइड्रा की शरीर की सतह से गैसों का आदान-प्रदान होता है।
यह प्रक्रिया विसरण (Diffusion) के माध्यम से होती है। - स्पंज (Sponge):
जल में रहने वाला प्राणी है। यह शरीर पर उपस्थित ऑस्ट्रिया नामक छिद्रों के माध्यम से घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है।
बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के प्रकार
| प्रकार | उदाहरण |
| त्वचीय श्वसन (Skin Respiration) | जोंक, केंचुआ, मेंढक (मूसलाधारित त्वचा) |
| ट्रेकियल श्वसन (Tracheal) | टिड्डा, चींटी, मधुमक्खी आदि (श्वासनली द्वारा) |
| गिल श्वसन (Gill Respiration) | मछली, झींगा (जल में रहने वाले जीव) |
तथ्य:
- तिलचट्टा के रक्त को हिमोलिम्फ (Hemolymph) कहा जाता है।
- हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है।
झींगा मछली का रंग सफेद क्यों होता है?
झींगा मछली के रक्त कणिकाओं में हेमोसाइएनिन (Hemocyanin) नामक प्रोटीन पाया जाता है।
- यह प्रोटीन ऑक्सीजन वाहक होता है
- इसमें कॉपर (तांबा) पाया जाता है, जिससे इसका रंग सफेद या हल्का नीला होता है।
पौधों और जन्तुओं में श्वसन में अंतर (Respiration in Plants vs Animals):
| विशेषता | पौधों में श्वसन | जंतुओं में श्वसन |
| गैसों का परिवहन | बहुत कम मात्रा में | अधिक मात्रा में |
| श्वसन की गति | धीमी | तीव्र |
| ऊर्जा की मात्रा | कम ऊर्जा उत्पन्न होती है | अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है |
किण्वन (Fermentation):
जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सेलिक अम्ल में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं।
किण्वन का स्थान:
- यह क्रिया यीस्ट (Yeast) जैसे सूक्ष्मजीवों में होती है।
किण्वन का उपयोग (Uses of Fermentation):
- शराब निर्माण में
- प्लास्टिक निर्माण में
- कपड़ा रंगाई में
- जूट उद्योग में
- तंबाकू उद्योग में
- खमीरयुक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन में (जैसे डोसा, इडली)
जैव रासायनिक क्रियाओं के प्रकार (Types of Biochemical Reactions)
सभी जीवों की कोशिकाओं में अत्यंत सूक्ष्म रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें जैव रासायनिक क्रियाएँ (Biochemical Reactions) कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं:
1. अपचयन (Catabolism):
जब जटिल कार्बनिक यौगिक (Complex Organic Compounds) टूटकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, तो इसे अपचयन कहा जाता है।
उदाहरण: श्वसन की प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है।
2. उपचयन (Anabolism):
जब सरल अकार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़कर जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसे उपचयन कहा जाता है।
उदाहरण: प्रकाश संश्लेषण — CO₂ और जल से ग्लूकोज का निर्माण।
ए.टी.पी. (ATP – Adenosine Triphosphate):
ATP एक विशेष प्रकार का जैव-रासायनिक यौगिक है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक (Carrier) तथा संग्राहक (Storage Molecule) होता है। इसे “ऊर्जा की मुद्रा” (Energy Currency) भी कहा जाता है।
ATP के कार्य (Functions of ATP):
- कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का संवहन करता है।
- विभिन्न रासायनिक यौगिकों का संश्लेषण ATP की सहायता से होता है।
- गति, संचलन, संकुचन जैसे कार्यों में ऊर्जा प्रदान करता है।
- तंत्रिका आवेग, पोषण, निष्कासन आदि क्रियाओं में सहायक है।
मानव श्वसन तंत्र (Human Respiratory System):
मानव श्वसन तंत्र उन सभी अंगों का समूह है जो श्वसन क्रिया (Respiration) में भाग लेते हैं और ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में सहायक होते हैं।

मुख्य श्वसन तंत्र (Main Respiratory System):
इसमें फेफड़े शामिल होते हैं।
- मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं जो हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं।
- प्रत्येक फेफड़ा एक थैली के आकार का होता है जिसकी भीतरी दीवारों पर रक्त वाहिकाओं (Blood Capillaries) का जाल बिछा होता है।
- फेफड़े वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित करके उसे रक्त के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं।
सहायक श्वसन तंत्र (Accessory Respiratory System):
ये अंग श्वसन प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन इसे सहज और सुरक्षित बनाते हैं। इनमें निम्नलिखित अंग शामिल हैं:
सहायक श्वसन तंत्र के अंग
1. नासिका (Nose):
- इसमें स्थित नासा गुहा की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती हैं जो 1–2 लीटर म्युकस का स्राव करती हैं।
- म्युकस में मौजूद चिपचिपे तत्व वायु में मौजूद धूलकणों और रोगाणुओं को रोकते हैं।
- नासिका छिद्रों के बाद की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं जो वायु को छानने का कार्य करते हैं।
- आगे का मार्ग नेसोफेरिंक्स (Nasopharynx) कहलाता है, जो नासा मार्ग और ग्रसनी को जोड़ता है।
2. कंठ (Larynx):
- पुरुषों में यह अधिक उभरा हुआ होता है।
- इसमें दो स्वर रज्जु (Vocal Cords) होते हैं जो कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
- कंठ के आगे का भाग श्वास नली (Trachea) कहलाता है।
3. फेफड़ों की संरचना:
- दोनों फेफड़ों में लगभग 700 मिलियन एल्विओलाई (कुपिकाएं) होती हैं।
- इन कुपिकाओं की भीतरी सतह पर शल्की एपिथीलियम ऊतक पाए जाते हैं जो गैसों के आदान-प्रदान में सहायक होते हैं।
4. डायाफ्राम (Diaphragm):
- यह एक लचीली परंतु मजबूत पेशी होती है जो वक्षीय गुहा (Thoracic Cavity) को पेटीय गुहा (Abdominal Cavity) से अलग करती है।
- श्वास लेते समय यह नीचे की ओर सिकुड़ती है, जिससे वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है और वायु अंदर आती है।
- श्वास छोड़ते समय यह ऊपर उठती है, जिससे फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है।
श्वसन प्रक्रिया के चरण (Stages of Respiration)
1 अंतः श्वसन (Inhalation):
जब वातावरण से वायु फेफड़ों के भीतर प्रवेश करती है, उसे अंतः श्वसन कहा जाता है।
इस प्रक्रिया के दौरान:
- डायाफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है
- वक्ष की पसलियां बाहर की ओर फैलती हैं
- पेट की पेशियां संकुचित होती हैं
➡ इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है।
2 वाह्य श्वसन (Exhalation):
जब फेफड़ों की भीतर की वायु बाहर निकलती है, तो उसे वाह्य श्वसन कहते हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान:
- डायाफ्राम ऊपर की ओर उठता है
- पसलियां अंदर की ओर झुकती हैं
- पेट की पेशियां दबाव डालती हैं
➡ इससे फेफड़े पिचक जाते हैं और वायु श्वास नली (Trachea) और नाक के माध्यम से बाहर निकल जाती है।
ध्यान दें: यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगभग 3 वर्ष लग जाते।
क्रेब्स चक्र (Krebs Cycle):
जब पाइरूविक अम्ल, कोशिका के माइट्रोकॉण्ड्रिया में उपस्थित एंजाइमों की सहायता से एक चक्रिय जैव-रासायनिक पथ से गुजरता है, तो इस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र कहा जाता है।
- यह चक्र ऊर्जा निर्माण की एक मुख्य प्रक्रिया है।
- इसका नाम सर हैन्स क्रेब्स के नाम पर रखा गया है।
इस चक्र के माध्यम से ATP, NADH और FADH₂ जैसे ऊर्जा यौगिक बनते हैं।
3. परिवहन (Transportation)
सजीवों में पोषक तत्व, गैसें, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ आदि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन (Transport) कहते हैं।

मानव परिवहन प्रणाली के भाग
1. रक्त (Blood):
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक (Connective Tissue) है, जो पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है:
A. प्लाज्मा (Plasma):
- यह रक्त का तरल भाग होता है।
- हल्के पीले रंग का चिपचिपा तरल होता है।
- यह रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है।
- इसमें:
- 90% जल
- 7% प्लाज्मा प्रोटीन
- खनिज लवण, हार्मोन, ग्लूकोज, यूरिया आदि घुले होते हैं।
B. रक्त कणिकाएं (Blood Corpuscles):
- लाल रक्त कणिकाएं (RBC):
- इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है।
- इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
- ये गैसों का परिवहन करती हैं।
- श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC):
- इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं।
- ये शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती हैं।
- इन्हें शरीर का “सुरक्षक” या “सिपाही” भी कहा जाता है।
- प्लेटलेट्स (Platelets):
- इनका कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है।
- इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति mm³ रक्त होती है।
- चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने में मदद करते हैं।
रक्त के कार्य (Functions of Blood)
रक्त एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में कई आवश्यक कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक लाता है, जहाँ से यह बाहर निकाल दी जाती है।
- यह पचे हुए भोजन से बने पोषक अणुओं को अवशोषण स्थल (जैसे छोटी आंत) से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
- यह शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बनाए रखने के लिए रोगाणुओं से लड़ने वाले तत्व (WBC) उपलब्ध कराता है।
- यह उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों (जैसे यूरिया) को कोशिकाओं से लेकर गुर्दों तक लाता है, जहाँ से वे मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं।
- यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और हार्मोनों को अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है।
रक्त वाहिकाओं के प्रकार (Types of Blood Vessels)
1. धमनियाँ (Arteries)
- ये वाहिनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं (फेफड़ों की धमनी को छोड़कर)।
- इनकी दीवारें मोटी, लचीली और कपाटहीन (valveless) होती हैं।
- इनमें रक्त का प्रवाह तेजी से और उच्च दबाव पर होता है।
- शरीर की सभी प्रमुख धमनी, महाधमनी (Aorta) से निकलती हैं।
2. शिराएँ (Veins)
- शिराएँ वे रक्त वाहिकाएँ हैं जो शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं।
- इनकी दीवारें पतली होती हैं और ये अक्सर त्वचा के नीचे पाई जाती हैं।
- इनमें कपाट (valves) होते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित होने में सहायता करते हैं।
- एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त ले जाती है, वह है फुफ्फुसीय शिरा (Pulmonary vein)।
3. रक्त कोशिकाएँ / केशिकाएँ (Capillaries)
- ये अत्यंत पतली रक्त नलिकाएं होती हैं, जो धमनी और शिराओं को जोड़ती हैं।
- ये कोशिकाओं के आस-पास एक जाल बनाती हैं जिससे गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का विनिमय (Exchange) होता है।
- इनके माध्यम से ही ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तथा अपशिष्ट उत्पाद बाहर आते हैं।
शुद्ध और अशुद्ध रक्त में अंतर
- शुद्ध रक्त: वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है और जो हृदय से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है।
- अशुद्ध रक्त: वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं और जो कोशिकाओं से फेफड़ों या गुर्दों की ओर लौटाया जाता है।
हृदय (Heart)
मनुष्य का हृदय एक शंक्वाकार पेशीय अंग है, जो फेफड़ों के बीच स्थित होता है और बायीं ओर कुछ झुका हुआ पाया जाता है। इसके मुख्य तथ्य:
- यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है।
- इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है।
- यह चार कक्षों (वेश्मों) में विभाजित होता है:
- दो ऊपरी कक्ष – आलिंद (Atria)
- दो निचले कक्ष – निलय (Ventricles)
- आलिंद की दीवारें पतली जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं।
हृदय की क्रियाएँ:
- यह रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाने के लिए पंप करता है।
- यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों और गुर्दों तक शुद्धि के लिए भेजता है।
- शुद्ध रक्त को पुनः शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है।
हृदय की गति:
- सिकुड़ने की क्रिया को सिस्टोल (Systole) कहते हैं।
- फैलने की क्रिया को डायस्टोल (Diastole) कहते हैं।
- सिस्टोल और डायस्टोल का एक चक्र मिलकर एक धड़कन बनाता है।
मनुष्य में दोहरा परिसंचरण (Double Circulation)
- रक्त को एक बार पूरे शरीर में घूमने के लिए दो बार हृदय से गुजरना पड़ता है।
- पहली बार, हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जाता है और शुद्ध होकर लौटता है – इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण (Pulmonary circulation) कहते हैं।
- दूसरी बार, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में जाता है – इसे शारीरिक परिसंचरण (Systemic circulation) कहते हैं।
- इसी कारण से, इसे दोहरा परिसंचरण (Double circulation) कहा जाता है।
रक्तचाप (Blood Pressure)
- जब रक्त, महाधमनी और उसकी शाखाओं में प्रवाहित होता है, तो वह दबाव डालता है।
- इस दबाव को रक्तचाप कहा जाता है।
हाइपरटेंशन (Hypertension)
- जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) कहा जाता है।
- यह हृदय, गुर्दे और मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है।
लसिका (Lymph)
लसिका एक पीले रंग का पारदर्शी द्रव होता है, जो रक्त का ही एक घटक है परंतु इसमें लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का अभाव होता है। इसमें मुख्य रूप से श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC) और जल होते हैं।
लसिका के कार्य:
- यह शरीर के ऊतकों में मौजूद अतिरिक्त जल को एकत्र कर उसे रक्त में वापस सम्मिलित करने का कार्य करता है।
- यह रोगाणुओं से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के माध्यम से शरीर की रक्षा करता है।
- यह कुछ कार्बनिक अम्लों और पोषक पदार्थों का निर्माण व परिवहन करता है।
- यह विशेष रूप से आंतों से वसा का अवशोषण कर उन्हें रक्त प्रवाह तक पहुँचाता है।
मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की औसत संख्या लगभग 5×10⁶ प्रति घन मिलीमीटर (mm³) पाई जाती है।
संवहन ऊतक (Conducting Tissues in Plants)
पेड़-पौधों में जल, खनिज और भोजन के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास हुआ है जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। इन ऊतकों के दो मुख्य प्रकार हैं: जाइलम और फ्लोएम।
1. जाइलम (Xylem)
- जाइलम उन ऊतकों को कहते हैं जो पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं।
- इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं।
- जाइलम में जल का बहाव केवल एक दिशा में यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है।
- यह पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है।
2. फ्लोएम (Phloem)
- फ्लोएम पौधों में बने खाद्य पदार्थों (ग्लूकोज आदि) का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में परिवहन करता है।
- इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं।
- फ्लोएम में भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है — ऊपर और नीचे।
- यह पौधे के विकासशील भागों जैसे फल, बीज, फूल व कली तक पोषण पहुंचाता है।
जाइलम और फ्लोएम में अंतर:
| विशेषता | जाइलम | फ्लोएम |
| कोशिकाएं | मृत | जीवित |
| परिवहन की दिशा | नीचे से ऊपर | ऊपर व नीचे दोनों |
| परिवहन का माध्यम | जल एवं खनिज | भोजन (ग्लूकोज) |
| प्रमुख कार्य | जल परिवहन | भोजन परिवहन |
पौधों में परिवहन की विधियाँ
स्थानांतरण (Translocation)
पौधों में खनिज एवं खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का एक भाग से दूसरे भाग में गति करना स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य मुख्यतः फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है।
वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)
पत्तियों की सतह पर मौजूद वातरंध्रों (stomata) से जल का भाप के रूप में वातावरण में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
- यह पौधे के शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
- वाष्पोत्सर्जन के कारण जाइलम में जल का खिंचाव उत्पन्न होता है जो जड़ों से जल ऊपर खींचता है।
चालनी नलिकाएं (Sieve Tubes)
- फ्लोएम के माध्यम से भोजन के परिवहन में जो कोशिकाएं कार्य करती हैं उन्हें चालनी नलिकाएं (Sieve tubes) कहा जाता है।
- ये जीवित कोशिकाएं होती हैं लेकिन इनमें नाभिक नहीं पाया जाता।
- चालनी नलिकाएं एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनकी सिरों पर चालनी जैसे छिद्र होते हैं जो भोजन के आवागमन में सहायक होते हैं।
4. उत्सर्जन (Excretion)
जीवों के शरीर के अंदर चयापचय की प्रक्रिया के दौरान अनेक अपशिष्ट व विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया को उत्सर्जन (Excretion) कहते हैं।

उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं के प्रकार
- एमीनोटेलिक (Ammonotelic):
वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं, एमीनोटेलिक कहलाते हैं।
उदाहरण: मछलियाँ, प्रोटोजोआ। - यूरियोटेलिक (Ureotelic):
वे जीव जो यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं।
उदाहरण: मेंढक, मनुष्य सहित सभी स्तनधारी। - यूरिकोटेलिक (Uricotelic):
वे जीव जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं।
उदाहरण: पक्षी, सरीसृप।
मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र
प्रमुख उत्सर्जी अंग:
1. वृक्क (Kidney):
- प्रत्येक मनुष्य में दो वृक्क (किडनी) होते हैं जिनका आकार सेम के बीज जैसा तथा रंग गहरा लाल-भूरा होता है।
- प्रत्येक किडनी में लगभग 1.3 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं।
- वृक्क दो भागों से मिलकर बना होता है: कॉर्टेक्स (बाहरी भाग) और मेडुला (भीतरी भाग)।
- प्रत्येक किडनी का औसत वजन लगभग 120 ग्राम होता है।
- वृक्क का कार्य रक्त को छानना, अवांछित पदार्थों को निकालना तथा मूत्र (Urine) बनाना है।
मूत्र (Urine) की विशेषताएं:
- मूत्र का pH मान 6 होता है।
- मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, जो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है।
- सामान्य मूत्र में 95% जल, 2.7% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल एवं 2% लवण होते हैं।
वृक्क (Kidney) के कार्य
- रक्त के प्लाज्मा को छानना और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना।
- रक्त से अवांछनीय नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट को मूत्र के रूप में निष्कासित करना।
- शरीर में जल संतुलन बनाए रखना।
- मूत्र के माध्यम से लवणों और अन्य अपशिष्ट रसायनों का निष्कासन।
मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंग:
- मूत्र वाहिनी (Ureter):
- प्रत्येक वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं।
- यह मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है।
- मूत्राशय (Urinary Bladder):
- यह एक नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना है।
- यह मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है।
- उदरगुहा के पिछले भाग में, रेक्टम के नीचे स्थित होता है।
- मूत्रमार्ग (Urethra):
- मूत्राशय के निचले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है।
- इसी मार्ग से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है।
- मूत्रमार्ग के त्रिकोणीय क्षेत्र को ट्राइगोन कहा जाता है।
अन्य संबंधित अवधारणाएँ
अपोहन (Dialysis):
- जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो रक्त को कृत्रिम रूप से छानने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं।
- इस प्रक्रिया में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बिना प्रोटीन को निकाले बाहर किया जाता है।
जल संतुलन (Water Balance):
- शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को जल संतुलन कहा जाता है।
- यह किडनी एवं अन्य अंगों की क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है।
अन्य उत्सर्जी अंगों की भूमिका
त्वचा (Skin):
- त्वचा में मौजूद स्वेट ग्लैंड (Sweat glands) पसीने के रूप में जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती हैं।
- यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी सहायक होती है।
फेफड़े (Lungs):
- श्वसन क्रिया के दौरान शरीर से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा किया जाता है।
- यह शरीर का मुख्य गैसीय उत्सर्जी पदार्थ है।
यकृत (Liver):
- यकृत शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को यूरिया व यूरिक अम्ल में बदलता है।
- यह वसा के पाचन में भी सहायक है।
मूत्र निर्माण की मात्रा का नियंत्रण
- मूत्र निर्माण की मात्रा शरीर की ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित होती है।
- यह निर्भर करता है:
- उत्सर्जी पदार्थों की सघनता पर
- शरीर में जल की मात्रा पर
- तंत्रिका आवेगों पर
- अपशिष्ट पदार्थ की प्रकृति पर
The End
अगर आपको यह कक्षा 10वीं जीव विज्ञान – अध्याय: जैव प्रक्रम : पोषण (Life Processes: Nutrition) के नोट्स उपयोगी लगे हों, तो ऐसे ही सरल, संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट StudyNumberOne.Co को जरूर विज़िट और फॉलो करें। यहाँ आपको कक्षा 10 के सभी विषयों — जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान आदि के नवीनतम और परीक्षा आधारित नोट्स मुफ्त में उपलब्ध हैं।