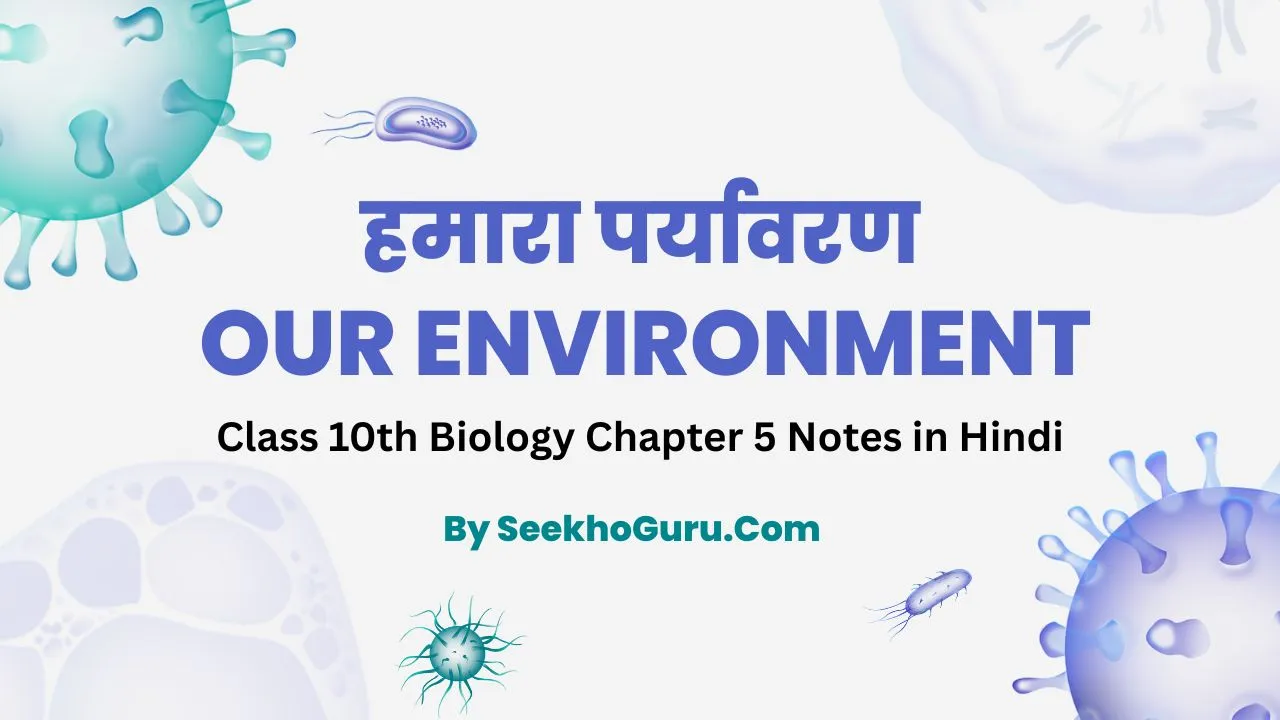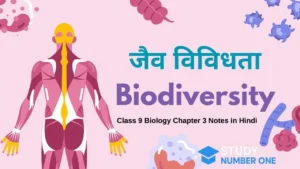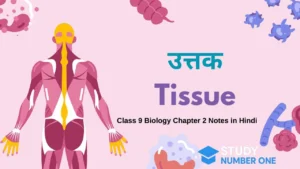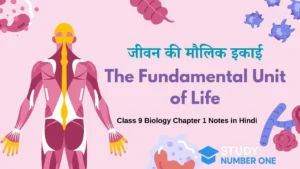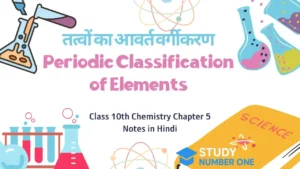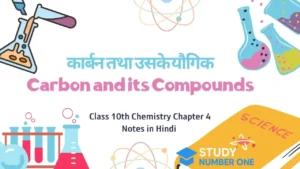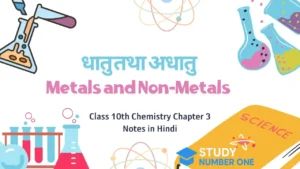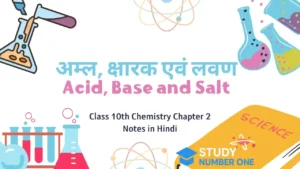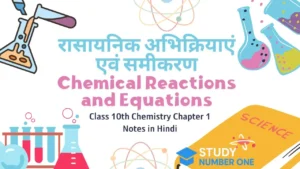Class 10th Biology Chapter 5 Notes in Hindi : मानव एवं पर्यावरण (Our Environment) के इस पोस्ट में हम आपको NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित, सरल, बोर्ड परीक्षा उपयोगी, और स्पष्ट हिंदी भाषा में तैयार मानव एवं पर्यावरण टॉपिक के सम्पूर्ण नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। यह नोट्स विशेष रूप से CBSE, Bihar Board, और अन्य राज्यों के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं ताकि वे इस अध्याय को आसानी से समझ सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें।
इसमें हमने आहार शृंखला, पोषी स्तर (Trophic Levels), ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, जैव आवर्धन (Biological Magnification), अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management), जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, ओजोन परत का क्षरण, और CFC जैसे रसायनों के प्रभाव को विस्तार से समझाया है। हर महत्वपूर्ण विषय को बोर्ड पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है ताकि यह छात्रों को परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के लिए पूरी तरह तैयार कर सके।
इस नोट्स में विषयों को चित्रों और बुलेट पॉइंट्स के साथ इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि यह तेजी से रिवीजन के लिए भी उपयुक्त है।
अगर आप Class 10th Science Chapter 5: मानव एवं पर्यावरण को एकदम स्पष्ट और आसान भाषा में समझना चाहते हैं और बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो यह फ्री नोट्स और PDF डाउनलोड आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
👉 अभी डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बनाएं आसान और प्रभावी।
Class 10th Biology Chapter 5 Notes in Hindi
पर्यावरण – Environment
किसी जीवधारी के चारों ओर फैला हुआ वह संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें भौतिक (जैसे मृदा, जल, वायु) और जैविक (जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव) घटक सम्मिलित होते हैं, और जो उस जीव के जीवन, विकास तथा व्यवहार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। यह वह प्राकृतिक और कृत्रिम स्थितियाँ हैं जिनके बीच जीव प्रतिदिन जीवन-यापन करता है।
¨ पर्यावरण के अंतर्गत –
- जलमंडल (Hydrosphere)
- स्थलमंडल (Lithosphere)
- वायुमंडल (Atmosphere)
- जीवमंडल (Biosphere)
शामिल होते हैं, जो मिलकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र – Ecosystem
जीवमंडल में मौजूद विभिन्न जैविक घटक जैसे – पौधे, जन्तु, मानव एवं सूक्ष्मजीव, जब मृदा, जल, वायु, ताप, प्रकाश जैसे अजैविक घटकों के साथ संपर्क में आते हैं और ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का आदान–प्रदान करते हैं, तो वह पूरा तंत्र पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) कहलाता है। यह तंत्र जैव एवं अजैव घटकों के बीच संतुलन, सहयोग और सहअस्तित्व पर आधारित होता है।
¨ पारिस्थितिक तंत्र एक स्वपोषी (self-sustained), संरचनात्मक (structural) और क्रियात्मक (functional) इकाई है, जो पर्यावरण में ऊर्जा और पोषक चक्र को बनाए रखती है।
¨ यह तंत्र ऊर्जा के लिए पूर्णतः सूर्य पर निर्भर रहता है, जहाँ से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
¨ इसके अजीव घटकों में –
मृदा, जल, वायु, ताप, और प्रकाश आते हैं,
जबकि जैव घटकों में –
पौधे, जन्तु, मानव, और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र की संरचना – Structure of Ecosystem
प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं, जो आपस में संपर्क में रहते हुए ऊर्जा, पोषक तत्वों, और सूचना का संचार करते हैं:
- (1) अजैव घटक (Abiotic Components)
- (2) जैव घटक (Biotic Components)
अजैव घटक – Abiotic Components
वे सभी गैर-जीवित तत्व जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उन्हें अजैव घटक कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है:
1. भौतिक वातावरण (Physical Environment)
इसमें मृदा (Soil), जल (Water) और वायु (Air) सम्मिलित होते हैं। ये तत्व जीवों के जीवन, विकास, और स्थान वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
2. पोषक तत्व (Nutrients)
इस श्रेणी में अकार्बनिक (Inorganic) जैसे खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बनिक (Organic) जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि तत्व आते हैं, जो विकास, ऊर्जा उत्पादन, और कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं।
3. जलवायवीय कारक (Climatic Factors)
इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता (Humidity), वायुदाब, और वायु की गति शामिल होती है, जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्माण करती हैं।
¨ जलवायु कारक जीवों की संख्या, स्थानिक वितरण (distribution), चयापचय (metabolism), और व्यवहार (behavior) पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और पूरे पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं।
जैव घटक – Biotic Components
पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले वे सभी सजीव घटक जो जीवन चक्र और ऊर्जा प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन्हें जैव घटक कहा जाता है। ये घटक ऊर्जा के उत्पादन, उपभोग, तथा अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन्हें निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँटा गया है –
- उत्पादक (Producers)
- उपभोक्ता (Consumers)
- अपघटनकर्ता (Decomposers)
1. उत्पादक – Producers
वे सभी जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इनका प्रमुख उदाहरण हरे पौधे हैं, जैसे शैवाल, घास, और वृक्ष, जिनमें प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया होती है।
¨ ऐसे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा (Light Energy) को क्लोरोफिल (Chlorophyll) की सहायता से रासायनिक स्थितिज ऊर्जा (Potential Chemical Energy) में परिवर्तित करते हैं, जो पौधों के ऊतकों में कार्बनिक यौगिक के रूप में संग्रहित होती है।
¨ यह ऊर्जा आगे चलकर खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाती है।
2. उपभोक्ता – Consumers
वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यह सभी जन्तु वर्ग को सम्मिलित करते हैं।
¨ उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है:
(i) प्राथमिक उपभोक्ता – Primary Consumers
ऐसे जीव जो सीधे हरे पौधों (Producers) को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये मुख्यतः शाकाहारी (Herbivores) होते हैं।
उदाहरण – गाय, बकरी, भैंस, हिरन, खरगोश, ग्रासहॉपर।
¨ कुछ जीव जैसे मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी (Omnivorous) होते हैं, यानी वे पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। जब वे केवल पौधों को खाते हैं, तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।
(ii) द्वितीयक उपभोक्ता – Secondary Consumers
वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये प्रायः मांसाहारी (Carnivorous) होते हैं।
उदाहरण – शेर, बाघ, मेंढक, साँप, कुछ पक्षी आदि।
(iii) तृतीयक उपभोक्ता – Tertiary Consumers
वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं।
उदाहरण – जब साँप, मेंढक (जो द्वितीयक उपभोक्ता है) को खाता है, तब साँप तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है।
¨ एक ही मांसाहारी जानवर विभिन्न परिस्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता बन सकता है।
उदाहरण –
- जब साँप, खरगोश को खाता है, तो वह द्वितीयक उपभोक्ता होता है।
- जब वही साँप, मेंढक को खाता है, तो वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है।
3. अपघटनकर्ता – Decomposers
वे सूक्ष्मजीव जो मृत उत्पादकों और उपभोक्ताओं के जैविक अवशेषों का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ये जीव मूलतः बैक्टीरिया और कवक (Bacteria & Fungi) होते हैं।
¨ ये मृत जीवों के जैविक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं और उससे उत्पन्न पोषक तत्वों और गैसों को पुनः वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे वे मृदा में पुनः उपलब्ध हो जाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र पूरा होता है।
आहार शृंखला –
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, और यह प्रवाह उस तंत्र में उपस्थित जीवों के शृंखलाबद्ध संबंधों के माध्यम से होता है। जीवों की इस ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली को ही आहार शृंखला (Food Chain) कहा जाता है।
¨ इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा को हरे पौधे (उत्पादक) द्वारा प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इसके पश्चात:
- उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी जीव) खाते हैं,
- फिर इन शाकाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता (मांसाहारी जीव) खाते हैं,
- अंत में इन्हें तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष शिकारी (Top Predators) द्वारा खाया जाता है।
¨ इस प्रकार, ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव तक केवल एक दिशा में होता है, और यह कभी भी वापस नहीं लौटता। इसी कारण इसे एकपथीय ऊर्जा प्रवाह (Unidirectional Flow of Energy) कहा जाता है।
कुछ सामान्य आहार शृंखलाएँ – Examples of Food Chains
- घास → ग्रासहॉपर → मेंढक → साँप → गिद्ध
- शैवाल → छोटे जलीय जीव → छोटी मछली → बड़ी मछली → मांसाहारी पक्षी
- पौधे → कृमि → चिड़िया → बिल्ली
- घास → हिरण → बाघ
आहार जाल – Food Web
प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आमतौर पर केवल एक ही आहार शृंखला नहीं होती, बल्कि अनेक जीवों के बीच कई आपस में जुड़ी हुई आहार शृंखलाएं पाई जाती हैं। ये शृंखलाएं अक्सर एक-दूसरे से आड़े-तिरछे जुड़ जाती हैं और एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। इन्हीं आपस में जुड़ी शृंखलाओं को आहार जाल (Food Web) कहा जाता है।
¨ आहार जाल पारिस्थितिक तंत्र को अधिक स्थिर और लचीला बनाता है, क्योंकि इसमें एक जीव के पास भोजन के कई स्रोत होते हैं और यह कई स्तरों पर ऊर्जा का आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है।
कुछ सामान्य आहार जाल उदाहरण – Food Web Examples
- पौधे → ग्रासहॉपर → बाज
- पौधे → ग्रासहॉपर → गिरगिट → बाज
- पौधे → खरगोश → बाज
- पौधे → चूहा → साँप → बाज
- पौधे → चूहा → बाज
पोषी स्तर – Trophic Level
किसी भी आहार शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न जीवों के बीच क्रमशः होता है। इस क्रम में, प्रत्येक जीव का एक निश्चित भोजन स्तर होता है जहाँ वह ऊर्जा प्राप्त करता है। आहार शृंखला में स्थित इन्हीं ऊर्जा स्थानांतरण स्तरों को पोषी स्तर (Trophic Level) कहा जाता है।
¨ एक सामान्य पारिस्थितिक तंत्र में प्रायः चार मुख्य पोषी स्तर पाए जाते हैं:
- प्रथम पोषी स्तर (Producers): इसमें हरे पौधे शामिल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश-संश्लेषण द्वारा भोजन में बदलते हैं।
- द्वितीय पोषी स्तर (Primary Consumers): इसमें शाकाहारी जीव जैसे हिरण, गाय, कीट आदि होते हैं, जो उत्पादकों को खाते हैं।
- तृतीय पोषी स्तर (Secondary Consumers): यह स्तर उन मांसाहारी जीवों का होता है जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक या साँप।
- चतुर्थ पोषी स्तर (Tertiary Consumers): इसमें शीर्ष शिकारी जैसे शेर, बाघ, या गिद्ध आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं।
¨ जैसे-जैसे हम पोषी स्तरों में ऊपर बढ़ते हैं, ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है।
पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार्य – Functions of Ecosystem
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रमुख प्रक्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं, जो उस तंत्र के संतुलन और अस्तित्व को बनाए रखती हैं।
(i) ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow):
हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह ऊर्जा फिर आहार शृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होती है। यह प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होता है — उत्पादक से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक।
(ii) पोषक तत्त्वों का चक्र (Nutrient Cycling):
जीवों की मृत्यु, अपघटन और अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से विभिन्न अजैव तत्त्व (जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल) वातावरण और जीवों के बीच चक्रीय रूप में घूमते रहते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र में संसाधनों की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है।
ऊर्जा प्रवाह – Energy Flow in Ecosystem
पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण एक विशेष 10% नियम (10 Percent Law) के अनुसार होता है। इसके अनुसार:
¨ किसी भी पोषी स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है।
¨ शेष 90% ऊर्जा उस जीव की शारीरिक क्रियाओं (जैसे श्वसन, गति, शरीर ताप नियंत्रित करना आदि) में नष्ट हो जाती है, या वातावरण में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है।
उदाहरण: यदि घास में 1000 यूनिट ऊर्जा है, तो घास खाने वाले हिरण को केवल 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसे खाने वाले शेर को केवल 10 यूनिट।
आहार शृंखला (Food Chain) :-
एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकपथीय होता है जो विभिन्न जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, जिससे एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनती है जिसे आहार शृंखला कहते हैं।
✦ सौर ऊर्जा सबसे पहले उत्पादक जीवों (हरे पौधे) द्वारा ग्रहण की जाती है।
✦ इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी जीव) खाते हैं।
✦ शाकाहारियों को द्वितीयक उपभोक्ता (मांसाहारी जीव) खाते हैं।
✦ अंत में इन मांसाहारियों को भी उच्च स्तरीय मांसाहारी (तृतीयक उपभोक्ता) खाते हैं।
इस प्रकार, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है – नीचे से ऊपर की ओर।
कुछ सामान्य आहार शृंखलाएँ:
- घास → ग्रासहॉपर → मेंढक → सर्प → गिद्ध
- शैवाल → छोटे जंतु → छोटी मछली → बड़ी मछली → मांसाहारी पक्षी
- पौधे → कृमि → चिड़िया → बिल्ली
- घास → हिरण → बाघ
आहार जाल (Food Web) :-
एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक आहार शृंखला नहीं होती, बल्कि कई आहार शृंखलाएँ एक साथ मौजूद होती हैं जो आपस में आड़ी-तिरछी जुड़ी होती हैं। जब ये मिलकर एक जाल का रूप ले लेती हैं, तो इसे आहार जाल कहते हैं।
उदाहरण:
- पौधे → ग्रासहॉपर → बाज
- पौधे → ग्रासहॉपर → गिरगिट → बाज
- पौधे → खरगोश → बाज
- पौधे → चूहा → सर्प → बाज
- पौधे → चूहा → बाज
पोषी स्तर (Trophic Level) :-
आहार शृंखला में मौजूद प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। हर पोषी स्तर पर भोजन (ऊर्जा) का स्थानांतरण होता है।
✦ प्रथम पोषी स्तर – उत्पादक जीव (हरे पौधे)
✦ द्वितीय पोषी स्तर – प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी)
✦ तृतीय पोषी स्तर – द्वितीयक उपभोक्ता (मांसाहारी)
✦ चतुर्थ पोषी स्तर – उच्च स्तरीय मांसाहारी (तृतीयक उपभोक्ता)
पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार्य (Functions of Ecosystem) :-
एक पारिस्थितिक तंत्र में दो मुख्य प्राकृतिक क्रियाएँ होती हैं:
(i) सबसे पहले सौर ऊर्जा का हरे पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है जो आगे अन्य जीवों को खाद्य रूप में प्राप्त होती है।
➤ यह ऊर्जा का प्रवाह एकपथीय होता है।
(ii) दूसरी प्रक्रिया में अजैविक पदार्थों का जैव और अजैव वातावरण के बीच चक्रीय आदान-प्रदान होता रहता है।
ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow) :-
आहार शृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा जीव की दैनिक गतिविधियों, गर्मी के रूप में या अन्य कार्यों में व्यय हो जाती है।
जैव आवर्धन (Biological Magnification) :-
जब हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि आहार शृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं और अंततः मानव शरीर में संग्रहीत हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं।
उदाहरण: DDT या अन्य रसायन फसलों में उपयोग किए जाते हैं और धीरे-धीरे आहार शृंखला के माध्यम से विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए मानव शरीर में पहुँच जाते हैं।
मानव एवं पर्यावरण (Human and Environment) :-
मनुष्य अपने दैनिक कार्यों के दौरान बहुत से अनावश्यक पदार्थ (कचरा) उत्पन्न करता है जिन्हें इधर-उधर फेंक दिया जाता है। इन्हें अपशिष्ट (waste) कहते हैं।
अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं:
(i) जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट (Biodegradable Waste):
ऐसे अवांछित पदार्थ जो जैविक अपघटन द्वारा फिर से उपयोग में लाए जा सकते हैं।
उदाहरण: कागज़, कपड़े, जानवरों के मल-मूत्र, पेड़-पौधों के मृत अंग, भोजन अवशेष आदि।
(ii) जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste):
ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं।
उदाहरण: प्लास्टिक, DDT, शीशा, एलुमिनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि।
कचरा प्रबंधन (Waste Management) :-
कचरे को एक जगह एकत्र कर, उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निपटान करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है।
ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय (Ozone Layer and Ozone Depletion) :-
ओजोन परत वायुमंडल में मौजूद एक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।
लेकिन, कुछ उत्पाद जैसे सुगंधित स्प्रे, कीटनाशक, शेविंग फोम आदि ऐरोसोल कहलाते हैं जिनमें प्रयुक्त CFC (Chlorofluorocarbons) गैसें ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं। इससे पृथ्वी पर ओजोन छिद्र बन जाता है और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो त्वचा रोग, कैंसर, पौधों को क्षति आदि का कारण बनता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
अगर आपको यह कक्षा 10वीं विज्ञान – अध्याय: मानव एवं पर्यावरण (Our Environment) के नोट्स उपयोगी लगे हों, तो ऐसे ही सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट Studynumberone.co को ज़रूर विज़िट और फॉलो करें।
यहाँ आपको कक्षा 10 के सभी विषयों — जीवविज्ञान (Biology), रसायनशास्त्र (Chemistry), भौतिकी (Physics), गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और सामाजिक विज्ञान आदि के NCERT आधारित नवीनतम और बोर्ड परीक्षा केंद्रित नोट्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं।
More Notes