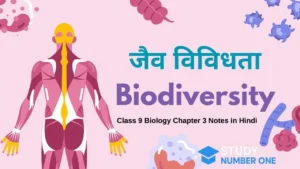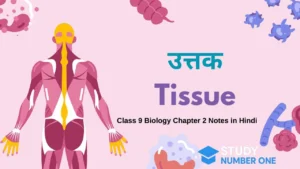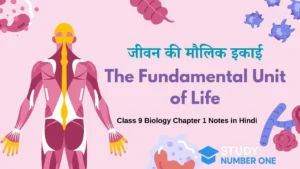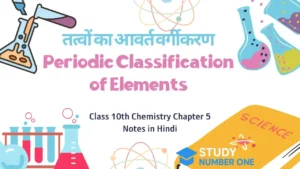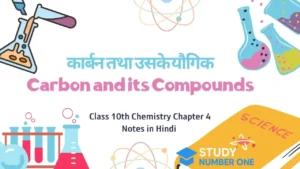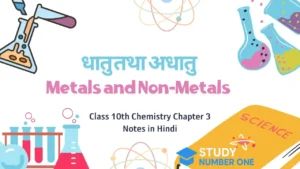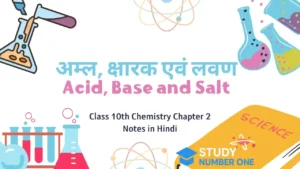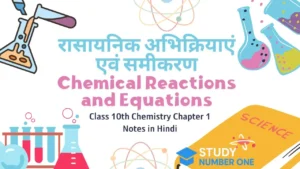Class 10th Physics Chapter 1 Notes in Hindi – प्रकाशः परावर्तन एवम् अपवर्तन (Light : Reflection and Refraction) के इस पोस्ट में हम आपको NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित, सरल, बोर्ड परीक्षा उपयोगी, और स्पष्ट हिंदी भाषा में तैयार सम्पूर्ण नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। यह नोट्स विशेष रूप से CBSE, Bihar Board, और अन्य राज्यों के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं ताकि वे इस अध्याय को आसानी से समझ सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें।
इसमें हमने परावर्तन के नियम, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के फोकस व फोकस दूरी, लेंस के प्रकार, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रतिबिंब के प्रकार, लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता और अपवर्तनांक जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से और बोर्ड पैटर्न के अनुसार समझाया है।
हर विषय को चित्रों, सारणियों और बुलेट पॉइंट्स के साथ इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि यह तेज़ी से रिवीजन के लिए भी उपयुक्त है।
अगर आप Class 10th Physics Chapter 1: Light – Reflection and Refraction को एकदम स्पष्ट और आसान भाषा में समझना चाहते हैं और बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो यह फ्री नोट्स और PDF डाउनलोड आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
अभी डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बनाएं आसान।
Class 10th Physics Chapter 1 Notes in Hindi
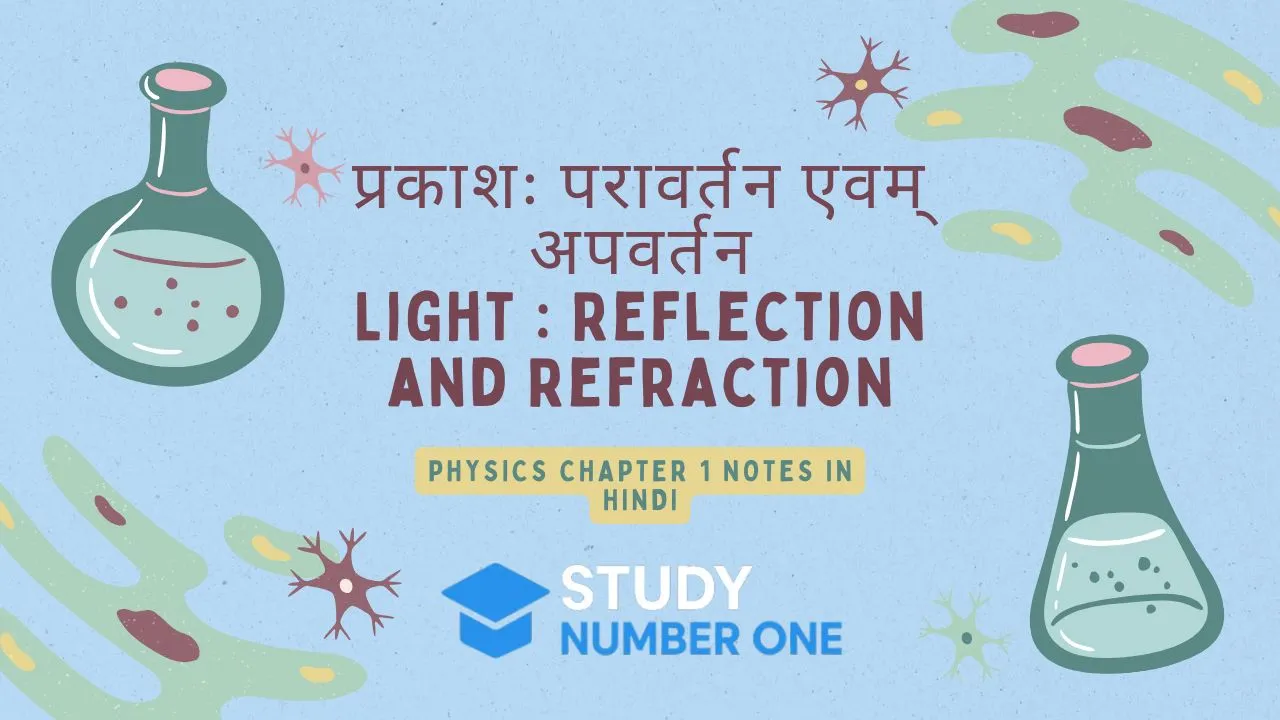
✸ प्रकाश (Light) :-
दुनिया की सभी वस्तुओं को देखने की क्षमता हमें एक विशेष ऊर्जा के कारण मिलती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों तक पहुँचकर दृश्य उत्पन्न करती है।
➤ वस्तुतः, जब यह ऊर्जा यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
✸ प्रकाश के गुण (Properties of Light) :-
➤ यह हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, जब तक कि इसे कोई माध्यम या सतह दिशा बदलने के लिए बाध्य न करे।
➤ यह विद्युत चुंबकीय तरंग (Electromagnetic Wave) है, इसलिए इसके प्रसार के लिए वायु, जल या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती — यह निर्वात में भी समान गति से चल सकता है।
➤ यह अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण और स्पष्ट छाया बनाता है, जिससे हमें वस्तु की आकृति का सटीक अनुमान मिल सकता है।
➤ निर्वात में इसकी चाल ब्रह्मांड की सबसे अधिक गति है – लगभग 3 × 10⁸ m/s, जो इसे ब्रह्मांड में सबसे तेज़ गति से यात्रा करने वाली इकाई बनाती है।
✸ प्रकाश – स्रोत (Light Source) :-
हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश का निर्माण और उत्सर्जन करती हैं, इन्हें प्रकाश-स्रोत कहते हैं।
➤ प्रकाश-स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –
- प्राकृतिक (Natural) – जैसे सूर्य, तारे आदि, जो ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
- मानव निर्मित (Man-Made) – जैसे मोमबत्ती, दीपक, लैम्प, बल्ब आदि, जिन्हें मनुष्य ने कृत्रिम रूप से बनाया है।
➤ प्रकाश-स्रोत ऊर्जा के अन्य रूपों को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं –
- (i) लालटेन और दीपक में तेल में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को दहन की प्रक्रिया से प्रकाश में बदला जाता है।
- (ii) बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को ताप और चमक उत्पन्न कर प्रकाश में बदला जाता है।
➤ इस प्रकार, प्रकाश एक विशिष्ट ऊर्जा का रूप है, जिसे अन्य ऊर्जाओं से उत्पन्न किया जा सकता है और यह जीवन के अनेक कार्यों के लिए आवश्यक है।
✸ प्रदीप्त (Luminous Things) :-
कुछ वस्तुएं अपने भीतर से प्रकाश उत्पन्न कर वातावरण को प्रकाशित करती हैं। इन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं।
➤ उदाहरण – सूर्य, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, तेल का दीपक आदि, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और आसपास की वस्तुओं को दिखाई देने योग्य बनाते हैं।
✸ अप्रदीप्त (Non-Luminous Things) :-
दुनिया में अधिकांश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करतीं, इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है।
➤ उदाहरण – मेज़, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि।
➤ हम इन वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश इन पर पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। बिना प्रकाश के, ये वस्तुएं हमारे लिए अदृश्य रहती हैं।
✸ प्रकीर्णन (Scattering) :-
जब प्रकाश की किरणें बहुत छोटे कणों या सूक्ष्म कणों पर गिरती हैं, तो वे कण उस प्रकाश का एक भाग अवशोषित (Absorb) कर लेते हैं और फिर उसे अलग-अलग दिशाओं में विकिरित (Radiate) कर देते हैं।
➤ इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यही कारण है कि दिन में आकाश नीला दिखाई देता है, सुबह और शाम को सूर्य का रंग लालिमा लिए होता है तथा धुंध या धूल में रोशनी फैली हुई प्रतीत होती है।
✸ प्रकाश की किरणें (Ray)
जब कोई प्रदीप्त वस्तु (Luminous Object) प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो वह प्रकाश सभी दिशाओं में सीधी रेखा में फैलता है।
➤ सीधी रेखा पर यात्रा करने वाली इस प्रकाश धारा को प्रकाश की किरण कहा जाता है। यह मूल रूप से प्रकाश का सबसे छोटा और सीधा पथ होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
✸ किरणपुंज (Beam)
प्रकाश की कई किरणें मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिसे किरणपुंज कहते हैं। यह एक दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों का संग्रह होता है।
➤ किरणपुंज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं –
(a) अपसारी किरणपुंज (Diverging Beam)
(b) समांतर किरणपुंज (Parallel Beam)
(c) अभिसारी किरणपुंज (Converging Beam)
(a) अपसारी किरणपुंज (Diverging Beam) :-
इस प्रकार के किरणपुंज में सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु-स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती हैं।
➤ उदाहरण के लिए, जलते बल्ब या मोमबत्ती से निकलने वाली रोशनी अपसारी किरणपुंज का रूप होती है।
(b) समांतर किरणपुंज (Parallel Beam) :-
इस प्रकार के किरणपुंज में सभी प्रकाश किरणें एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं और उनके बीच की दूरी स्थिर रहती है।
➤ बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश-स्रोत (जैसे – सूर्य) से आने वाली किरणों को हम लगभग समांतर मान सकते हैं, क्योंकि इतनी दूरी पर उनके बीच का कोण नगण्य होता है।
(c) अभिसारी किरणपुंज (Converging Beam) :-
इस प्रकार के किरणपुंज में सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
➤ ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है, जैसे किसी लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश का किसी बिंदु पर केंद्रित होना।
✸ पारदर्शी पदार्थ (Transparent)
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे होकर प्रकाश लगभग बिना किसी रुकावट के गुजर जाता है। इन्हें पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है।
➤ उदाहरण – साफ कांच, स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा आदि।
➤ इन पदार्थों से गुजरते समय प्रकाश की दिशा में बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनके आर-पार वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं।
✸ पारभासी पदार्थ (Translucent)
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के केवल एक हिस्से को अपने आर-पार जाने देते हैं।
➤ इनसे गुजरते हुए प्रकाश बिखर जाता है, जिससे इनके पीछे की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं।
➤ उदाहरण – घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, गुब्बारे का पतला रबर, आंख की पलक, हल्के बादल, कुहासा आदि।
✸ अपारदर्शी पदार्थ (Opaque)
कुछ वस्तुएं प्रकाश को बिल्कुल भी अपने आर-पार नहीं जाने देतीं। ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है।
➤ इन पर प्रकाश पड़ने पर यह या तो उसे परावर्तित (Reflect) कर देते हैं या अवशोषित (Absorb) कर लेते हैं।
➤ उदाहरण – लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट आदि।
✸ प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light)
जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
➤ चिकनी और अच्छी तरह पॉलिश की गई सतहों पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश उनकी सतह से परावर्तित होकर लौट जाता है।
➤ समतल दर्पण (Plane Mirror) प्रकाश का उत्कृष्ट परावर्तक होता है।
➤ एक समतल दर्पण पारदर्शी कांच की सपाट प्लेट होती है, जिसकी पीछे की सतह पर परावर्तक परत चढ़ाई जाती है।
➤ प्रकाश की किरणों का पथ और दिशा दर्शाने वाले चित्र को किरण-आरेख (Ray Diagram) कहा जाता है।
✸ परावर्तन के नियम (Laws of Reflection)
जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरकर वापस लौटती है, तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। इन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है।
➤ इन नियमों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद (Terms) निम्नलिखित हैं –
- आपतित किरण (Incident Ray) :-
सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण, जो किसी विशेष बिंदु पर सतह से टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। - आपतन बिंदु (Point of Incidence) :-
सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। - परावर्तित किरण (Reflected Ray) :-
सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। - अभिलम्ब (Normal) :-
किसी सतह के आपतन बिंदु पर उस सतह के लंबवत खींची गई कल्पित रेखा को अभिलम्ब कहते हैं। - आपतन कोण (Angle of Incidence) :-
आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। - परावर्तन कोण (Angle of Reflection) :-
परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम
(i) आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलम्ब — तीनों हमेशा एक ही समतल में स्थित होते हैं।
(ii) आपतन कोण (i) और परावर्तन कोण (r) का मान हमेशा समान होता है, अर्थात i = r।
✸ प्रतिबिंब (Image)
जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी बिंदु से आ रही हैं, तो उस बिंदु को बिंदु-स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है।
प्रतिबिंब के प्रकार
प्रकाश के परावर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं –
- वास्तविक प्रतिबिंब (Real Image)
➤ जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो बनने वाले चित्र को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है।
➤ वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे (Screen) पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
➤ यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा (Inverted) होता है। - आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब (Virtual Image)
➤ जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वहां नहीं होतीं, तो बनने वाले चित्र को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है।
➤ आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
➤ यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा (Erect) होता है।
✸ पार्श्व परिवर्तन (Lateral Inversion)
जब किसी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बाएँ भाग के रूप में और बायाँ भाग दाएँ भाग के रूप में दिखाई देता है, तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है।
यह प्रभाव समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की एक विशेषता है।
✸ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएँ
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –
(i) प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है।
(ii) प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है।
(iii) प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है।
(iv) प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है।
(v) प्रतिबिंब हमेशा आभासी (Virtual) होता है।
(vi) प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है।
✸ गोलीय दर्पण (Spherical Mirror)
ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है।
इन दर्पणों की सतह चिकनी और परावर्तक होती है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं – अवतल दर्पण (Concave Mirror) और उत्तल दर्पण (Convex Mirror)।
✦ गोलीय दर्पण के प्रकार
गोलीय दर्पणों को उनकी परावर्तक सतह की दिशा के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है –
(i) अवतल दर्पण (Concave Mirror)
➤ ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर, अर्थात गोले के केंद्र की ओर मुड़ी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है।
➤ यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित (Converge) करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे विभिन्न वैज्ञानिक, चिकित्सीय और दैनिक उपयोग में लिया जाता है।
उपयोग:
(A) दाढ़ी बनाने में चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब पाने के लिए।
(B) नेत्र, दंत, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें संबंधित अंग पर केंद्रित हो जाती हैं।
(C) टेबल लैम्प में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए।
(D) मोटरकारों, रेल इंजनों और सर्च लाइट के लैंप में परावर्तक (Reflector) के रूप में।
(ii) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)
➤ ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है।
➤ यह प्रकाश की किरणों को अपसारित (Diverge) करता है, और अधिक क्षेत्र (Wide View) का दृश्य प्रदान करता है।
उपयोग:
(A) मोटरकारों में ड्राइवर की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने (Rear View Mirror) के लिए।
(B) सड़क के मोड़ों और पार्किंग एरिया में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जिससे व्यापक क्षेत्र दिखाई दे।
अतिरिक्त तथ्य:
➤ काँच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित (Silvered) करने पर अवतल दर्पण बनता है।
➤ काँच के टुकड़े की भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण बनता है।
✸ गोलीय दर्पण से सम्बंधित विभिन्न पद (Terms)
- ध्रुव (Pole)
➤ दर्पण की सतह के मध्य में स्थित बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यह दर्पण के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। - वक्रता केंद्र (Centre of Curvature)
➤ वह बिंदु जो उस काल्पनिक गोले का केंद्र होता है, जिसका भाग दर्पण की परावर्तक सतह है। - वक्रता–त्रिज्या (Radius of Curvature)
➤ दर्पण जिस काल्पनिक गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या को वक्रता–त्रिज्या कहते हैं। - प्रधान या मुख्य अक्ष (Principal Axis)
➤ ध्रुव और वक्रता–केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है।
✸ गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी
➤ किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह विशिष्ट बिंदु, जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित (मिल) होती हैं, फोकस कहलाता है।
➤ उत्तल दर्पण के मामले में, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपसारित (फैल) होती हैं और उनका प्रत्यक्ष (Virtual) संगम बिंदु फोकस माना जाता है।
➤ दर्पण के ध्रुव (Pole) और मुख्य फोकस (Principal Focus) के बीच की दूरी को फोकस दूरी (Focal Length) कहते हैं। इसे अक्षर F से निरूपित किया जाता है।
➤ छोटे आकार के गोलीय दर्पणों के लिए, वक्रता त्रिज्या (R) फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जिसे गणितीय रूप में –
R=2F
द्वारा व्यक्त करते हैं।
➤ साधारण शब्दों में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता–त्रिज्या का आधा होती है।
✦ गोलीय दर्पण में किरणों का परावर्तन और प्रतिबिंब निर्माण के नियम
- मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
➤ अवतल दर्पण में – परावर्तन के बाद यह किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है।
➤ उत्तल दर्पण में – परावर्तन के बाद यह किरण ऐसे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जो दर्पण का मुख्य फोकस है। - मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण
➤ अवतल दर्पण में – परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
➤ उत्तल दर्पण में – मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। - वक्रता–केंद्र से होकर आने वाली किरण
➤ अवतल दर्पण में – यह किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है।
➤ उत्तल दर्पण में – वक्रता–केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौटती है। - मुख्य अक्ष से तिर्यक (Oblique) दिशा में आने वाली किरण
➤ दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आने वाली किरण परावर्तन के बाद भी तिर्यक दिशा में ही जाती है और आपतन बिंदु पर आपतित व परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं।
✸ गोलीय दर्पण में प्रयुक्त चिह्न
➤ P – दर्पण का ध्रुव (Pole)
➤ PC – दर्पण का मुख्य अक्ष (Principal Axis)
➤ C – वक्रता–केंद्र (Centre of Curvature)
➤ AB – मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु
➤ F – मुख्य फोकस (Principal Focus)
➤ A’B’ – मुख्य अक्ष पर बनी वस्तु का प्रतिबिंब
✸ चिह्न परिपाटी (Sign Convention)
प्रकाशिकी में, दर्पण से वस्तु की दूरी (u), दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी (v), तथा फोकस दूरी (f) को सही दिशा के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक चिह्न दिए जाते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है, जो इस प्रकार है –
➤ वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं।
➤ सभी दूरियाँ मुख्य अक्ष के साथ दर्पण के ध्रुव (Pole) से मापी जाती हैं।
➤ यदि कोई दूरी मूल बिंदु के दाईं ओर (+x-अक्ष की दिशा) मापी जाए, तो उसे धनात्मक माना जाता है।
यदि दूरी मूल बिंदु के बाईं ओर (–x-अक्ष की दिशा) मापी जाए, तो उसे ऋणात्मक माना जाता है।
➤ यदि दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर (+y-अक्ष की दिशा) मापी जाए, तो वह धनात्मक होगी।
यदि दूरी मुख्य अक्ष के नीचे (–y-अक्ष की दिशा) मापी जाए, तो वह ऋणात्मक होगी।
➤ इस परिपाटी के अनुसार –
(i) अवतल दर्पण की वक्रता–त्रिज्या (R) और फोकस–दूरी (F) ऋणात्मक होती है।
(ii) उत्तल दर्पण की वक्रता–त्रिज्या (R) और फोकस–दूरी (F) धनात्मक होती है।
✸ दर्पण सूत्र (Mirror Formula)
➤ वस्तु दूरी (Object Distance) – ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे u से निरूपित किया जाता है।
➤ प्रतिबिंब दूरी (Image Distance) – ध्रुव P से प्रतिबिंब I की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे v से निरूपित किया जाता है।
➤ फोकस दूरी (Focal Length) – ध्रुव P से फोकस F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से निरूपित किया जाता है।
➤ वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature) – ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से निरूपित किया जाता है।
➤ दर्पण सूत्र –
गोलाकार दर्पण के लिए, वस्तु दूरी (u), प्रतिबिंब दूरी (v), और फोकस दूरी (f) के बीच संबंध इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है –
✸ आवर्धन (Magnification)
➤ प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्धन (Magnification) कहते हैं।
➤ इसे m से निरूपित किया जाता है।
➤ सूत्र –
(i) रैखिक आवर्धन (Linear Magnification)
(ii) दर्पण के लिए
✸ प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light)
परिभाषा:
➤ प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
✸ प्रकाश की चाल (Speed of Light)
➤ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है।
➤ निर्वात/शून्य में गति: लगभग 300,000 km/s (तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड)।
➤ जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व (Optical Density) अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है।
➤ यदि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, तो दूसरा माध्यम प्रकाशतः सघन (Optically Denser) और पहला माध्यम प्रकाशतः विरल (Optically Rarer) कहलाता है।
✸ अपवर्तनांक (Refractive Index)
➤ किसी माध्यम की, प्रकाश की दिशा को बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं।
सूत्र:
जहाँ,
- n = अपवर्तनांक
- c = निर्वात में प्रकाश की चाल
- v = उस माध्यम में प्रकाश की चाल
✸ आपेक्षिक अपवर्तनांक (Relative Refractive Index)
➤ दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं।
✦ अपवर्तन के नियम (Laws of Refraction)
- आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण – तीनों एक ही समतल में होते हैं।
- किसी विशेष माध्यम युग्म और विशेष वर्ण के लिए sin i/sin r का अनुपात नियतांक होता है।
➤ यही स्नेल का नियम (Snell’s Law) है।
✸ दैनिक जीवन में अपवर्तन के प्रभाव
(i) जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है।
(ii) जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है।
(iii) यदि प्रकाश की किरण दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत गिरे, तो वह दिशा बदले बिना सीधे निकल जाती है।
✸ प्रिज्म (Prism)
➤ किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं।
➤ जिन दो सतहों से प्रकाश का आवागमन होता है, उन्हें अपवर्तक पृष्ठ (Refracting Faces) कहते हैं।
➤ अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण (Angle of Prism) कहते हैं।
➤ आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण (Angle of Deviation) कहते हैं।
➤ अपवर्तक कोण अधिक होने पर, विचलन कोण भी अधिक होता है।
✸ लेंस (Lens)
➤ पारदर्शी तथा समरूप (Homogeneous) पदार्थ का ऐसा ठोस टुकड़ा, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों (आमतौर पर गोलीय सतहों) से घिरा होता है और जिससे होकर प्रकाश किरणें गुजरने पर अपवर्तन का अनुभव करती हैं, उसे लेंस कहा जाता है। लेंस प्रकाश की दिशा को बदलने, किरणों को अभिसरित (Converge) या अपसारित (Diverge) करने में सक्षम होते हैं।
✦ लेंस के प्रकार
लेंस को उनकी संरचना और सतहों के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है –
- उत्तल लेंस (Convex Lens)
➤ इसका मध्य भाग किनारों की तुलना में अधिक मोटा होता है। जब समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से गुजरती हैं, तो वे एक बिंदु पर इकट्ठी (अभिसरित) हो जाती हैं। इस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। - अवतल लेंस (Concave Lens)
➤ इसमें किनारे मध्य भाग की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। जब समानांतर प्रकाश किरणें इस लेंस से होकर गुजरती हैं, तो वे फैलकर (अपसारित होकर) अलग-अलग दिशाओं में चली जाती हैं। इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
✦ उत्तल लेंस के प्रकार
(i) उभयोत्तल (Biconvex) – जिसके दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी हुई हों।
(ii) समतलोत्तल (Plano-convex) – जिसमें एक सतह समतल हो और दूसरी सतह उत्तल हो।
(iii) अवतलोत्तल (Concavo-convex) – जिसमें एक सतह उत्तल और दूसरी सतह अवतल हो।
✦ अवतल लेंस के प्रकार
(i) उभयावतल (Biconcave) – जिसके दोनों सतहें भीतर की ओर धँसी हुई (अवतल) हों।
(ii) समतलावतल (Plano-concave) – जिसमें एक सतह समतल और दूसरी सतह अवतल हो।
(iii) उत्तलावतल (Convexo-concave) – जिसमें एक सतह उत्तल और दूसरी सतह अवतल हो, लेकिन उत्तल सतह का वक्रण कम हो।
✸ वक्रता–केंद्र (Centre of Curvature)
➤ लेंस की सतहें जिन कल्पित गोलों का भाग होती हैं, उनके केंद्रों को वक्रता–केंद्र कहा जाता है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता–केंद्र होते हैं — प्रत्येक सतह के लिए एक।
✸ मुख्य अक्ष (Principal Axis)
➤ लेंस के दोनों वक्रता–केंद्रों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह लेंस का केंद्रीय संदर्भ रेखा होती है, जिसके सापेक्ष सभी दूरी और कोण मापे जाते हैं।
✸ प्रकाश–केंद्र (Optical Centre)
➤ लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह विशिष्ट बिंदु, जिससे होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद अपनी दिशा बदले बिना सीधे निकल जाती है, प्रकाश–केंद्र कहलाता है।
✦ लेंस की क्रिया
- उत्तल लेंस – इस प्रकार का लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जिससे यह अभिसारी लेंस कहलाता है।
- अवतल लेंस – इस प्रकार का लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को फैलाता है, जिससे यह अपसारी लेंस कहलाता है।
✸ फोकस एवं फोकस–दूरी (Focus and Focal Length)
➤ जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु F₁ से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से होकर अपवर्तित होती हैं और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु F₁ को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस (First Principal Focus) कहा जाता है।
➤ इसी प्रकार, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु F₁ की दिशा में जब प्रकाश किरणें आती हैं और लेंस से होकर अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है।
➤ लेंस के प्रकाश–केंद्र (Optical Centre) O से प्रथम मुख्य फोकस F₁ तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस–दूरी कहते हैं।
➤ यदि समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी उत्तल लेंस से गुजरें, तो वे अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु F₂ से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस (Second Principal Focus) कहा जाता है।
➤ अवतल लेंस के लिए, समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद ऐसे फैलती हैं मानो वे किसी निश्चित बिंदु F₂ से आ रही हों; इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं।
➤ प्रकाश–केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस–दूरी कहा जाता है।
➤ सामान्य रूप से, लेंस के प्रकाश–केंद्र से किसी भी फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस–दूरी (Focal Length) कहा जाता है।
➤ लेंस की सतहों की वक्रता जितनी अधिक होती है (अर्थात लेंस जितना मोटा होता है), उसकी फोकस–दूरी उतनी ही कम होती है।
➤ उत्तल लेंस की फोकस–दूरी को धनात्मक (+) मानते हैं।
➤ अवतल लेंस की फोकस–दूरी को ऋणात्मक (–) मानते हैं।
✸ प्रतिबिंब (Image)
➤ किसी बिंदु–स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस से होकर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है।
प्रतिबिंब के प्रकार
- वास्तविक प्रतिबिंब (Real Image)
➤ वह स्थिति, जिसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है।
➤ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। - आभासी प्रतिबिंब (Virtual Image)
➤ वह स्थिति, जिसमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाती है।
➤ आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में सीधा होता है।
➤ उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के दोनों प्रकार के प्रतिबिंब (वास्तविक और आभासी) बन सकते हैं।
➤ अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है।
✸ लेंसों के लिए निर्देशांक चिह्न (Sign Convention for Lenses)
(i) लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष XX′ माना जाता है।
(ii) सभी दूरियाँ लेंस के प्रकाश–केंद्र से मापी जाती हैं।
(iii) आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक (Positive) मानी जाती हैं, जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक (Negative) मानी जाती हैं।
(iv) मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियाँ, यदि अक्ष के ऊपर हों तो धनात्मक और यदि अक्ष के नीचे हों तो ऋणात्मक मानी जाती हैं।
✸ लेंस सूत्र (Lens Formula)
➤ किसी लेंस के लिए वस्तु–दूरी (u), प्रतिबिंब–दूरी (v) और फोकस–दूरी (f) के बीच एक निश्चित गणितीय संबंध होता है। इस संबंध को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है।
लेंस सूत्र इस प्रकार है —
जहाँ,
(i) वस्तु–दूरी (u) → प्रकाश–केंद्र L से वस्तु O तक की दूरी को वस्तु–दूरी कहते हैं। इसे u से निरूपित किया जाता है।
(ii) प्रतिबिंब–दूरी (v) → प्रकाश–केंद्र L से प्रतिबिंब I तक की दूरी को प्रतिबिंब–दूरी कहते हैं। इसे v से निरूपित किया जाता है।
(iii) फोकस–दूरी (f) → प्रकाश–केंद्र L से लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस F₂ तक की दूरी को फोकस–दूरी कहते हैं। इसे f से निरूपित किया जाता है।
➤ इन तीनों दूरी के मापन में निर्देशांक चिह्न नियम (Sign Convention) का पालन करना आवश्यक होता है।
✸ आवर्धन (Magnification)
➤ किसी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है।
यदि,
- वस्तु की ऊँचाई = h
- प्रतिबिंब की ऊँचाई = h′
तो,
इसके अलावा, आवर्धन को दूरी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है —
आवर्धन के चिह्न का महत्व
- m का ऋणात्मक (–) मान → प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है, अर्थात यह वास्तविक प्रतिबिंब है।
- m का धनात्मक (+) मान → प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा होता है, अर्थात यह आभासी प्रतिबिंब है।
✸ लेंस की क्षमता (Power of a Lens)
➤ किसी लेंस की क्षमता (P) उसकी फोकस–दूरी (f) के व्युत्क्रम के बराबर होती है।
➤ क्षमता का SI मात्रक मीटर⁻¹ (m⁻¹) होता है, जिसे डायोप्टर (D) कहते हैं।
➤ 1 डायोप्टर (1 D) उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस–दूरी 1 मीटर हो।
निष्कर्ष (Conclusion):
अगर आपको यह कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान – अध्याय: प्रकाशः परावर्तन एवम् अपवर्तन (Light : Reflection and Refraction) के नोट्स उपयोगी लगे हों, तो ऐसे ही सरल, संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट StudyNumberOne.co को जरूर विज़िट और फॉलो करें।
यहाँ आपको कक्षा 10 के सभी विषयों — भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान आदि के नवीनतम और बोर्ड परीक्षा आधारित नोट्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं।
Study Number One – जहाँ पढ़ाई आसान होती है।