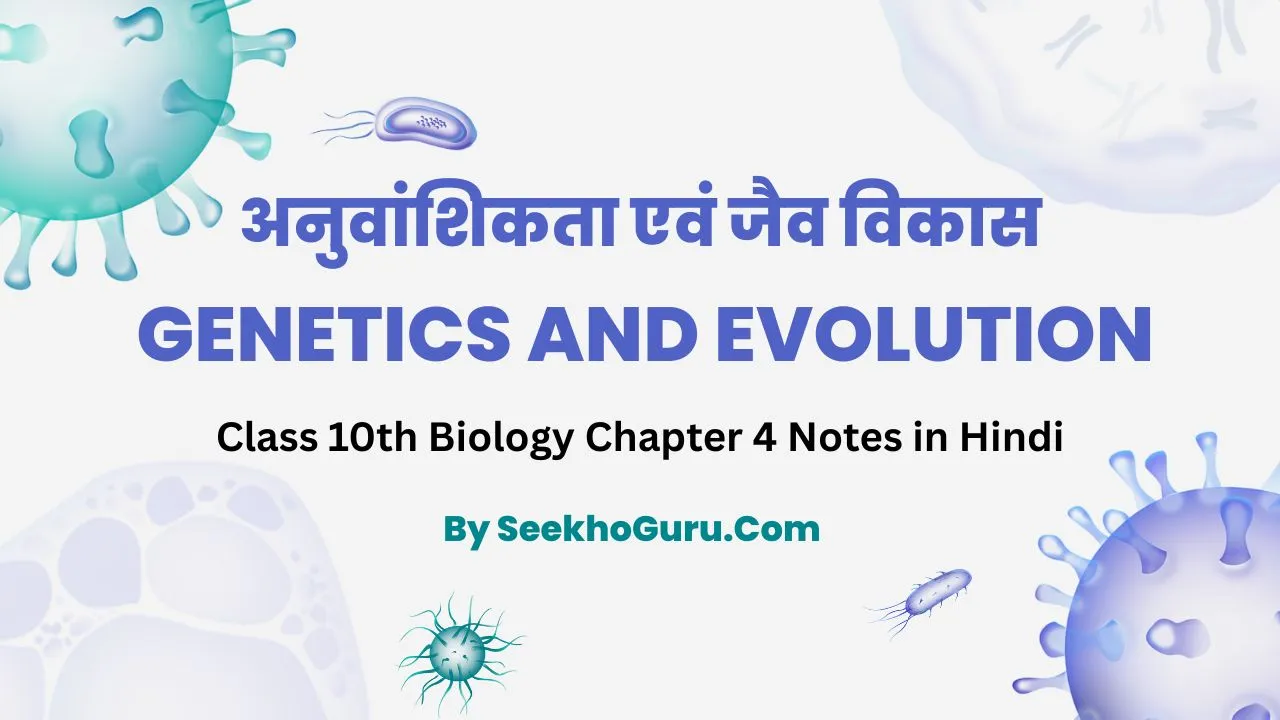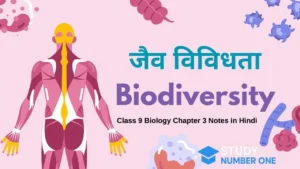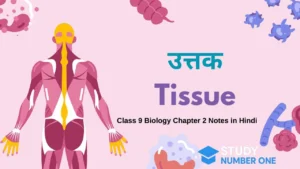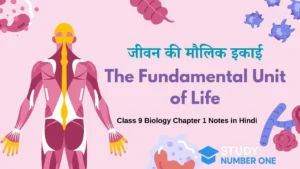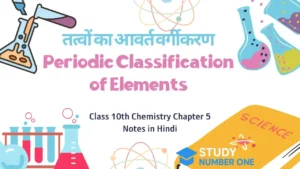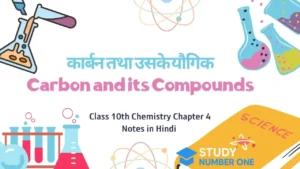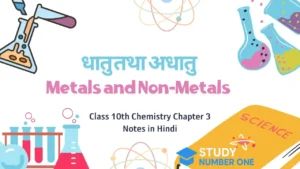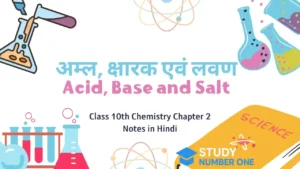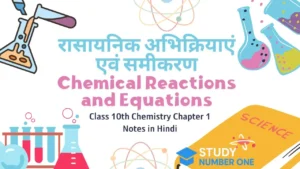Class 10th Biology Chapter 4 Notes in Hindi – अनुवांशिकता एवं जैव विकास (Genetics and Evolution) के इस पोस्ट में हम आपको पूरी तरह से NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित, सरल और स्पष्ट हिंदी भाषा में तैयार इस अध्याय के सम्पूर्ण नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। यह नोट्स खासतौर पर CBSE, Bihar Board और अन्य राज्यों के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे वे इस अध्याय को आसानी से समझ सकें और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
इसमें वंशागति (Heredity), मेंडल के नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम, F2 पीढ़ी में लक्षणों का 9:3:3:1 अनुपात, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत, समजात एवं असमजात अंगों का विश्लेषण, जीवाश्म के उदाहरण, रेडियोकार्बन काल-निर्धारण, तथा DNA अनुक्रम के आधार पर आण्विक जातिवृत (Molecular Phylogeny) जैसे सभी प्रमुख विषयों को विस्तार से समझाया गया है। साथ ही, इसमें पाठ्यपुस्तक के अनुसार चित्रों और चार्ट्स की मदद से विषय को और भी स्पष्ट किया गया है।
अगर आप Class 10th Biology Chapter 4: Genetics and Evolution को आसान भाषा में समझना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो यह फ्री नोट्स और PDF डाउनलोड आपके लिए बिल्कुल सही है।
👉 अभी डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बनाएं और भी आसान और मजबूत।
Class 10th Biology Chapter 4 Notes in Hindi
विभिन्नताएं (Variation)
विभिन्नता जीव के उन गुणों को दर्शाती है जो उसे उसके जनकों (माता-पिता) अथवा उसकी ही जाति (species) के अन्य सदस्यों से किसी विशेष गुण के संदर्भ में अलग बनाती है। ये अंतर कभी-कभी सूक्ष्म होते हैं लेकिन जीवों के विकास और अनुकूलन में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
विभिन्नताओं के प्रकार :
विभिन्नताएं दो प्रमुख प्रकार की होती हैं –
- जननिक विभिन्नता (Germinal Variation)
- कायिक विभिन्नता (Somatic Variation)
1. जननिक विभिन्नता (Germinal Variation) :-
यह ऐसी विभिन्नता होती है जो जनन कोशिकाओं (gametes) में होने वाले परिवर्तन या उत्परिवर्तन (mutation) के कारण उत्पन्न होती है।
➤ ये विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं, अर्थात् एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं।
➤ ये परिवर्तन डीएनए (DNA) में होते हैं और संतान के लक्षणों को प्रभावित करते हैं।
➤ ये जन्म से ही प्रकट हो सकते हैं, जैसे –
▪ आँखों का रंग
▪ बालों का रंग
▪ शारीरिक संरचना
▪ त्वचा का रंग
▪ शरीर की लंबाई
▪ कानों का आकार आदि।
➤ ये स्थायी होती हैं और वंश में आगे भी बनी रहती हैं।
2. कायिक विभिन्नता (Somatic Variation) :-
यह ऐसी विभिन्नता होती है जो जीव के शरीर की सामान्य कोशिकाओं में उत्पन्न होती है और इसके लिए कई बाह्य कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे –
▪ जलवायु परिवर्तन
▪ खानपान की आदतें
▪ जीवनशैली
▪ रोगों का प्रभाव
▪ शरीर पर लगी चोट या बीमारी
➤ ऐसी विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होतीं।
➤ ये केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहती हैं और संतानों में स्थानांतरित नहीं होतीं।
➤ इन्हें उपार्जित लक्षण (acquired characters) कहा जाता है।
➤ उदाहरण के लिए — किसी व्यक्ति की मांसपेशियों का विकास व्यायाम से हुआ हो, या सूर्य की तेज़ रोशनी में काम करने से त्वचा का रंग गहरा हो गया हो।
आनुवंशिकता (Heredity)
जब जनकों के गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों (gametes) के माध्यम से संचारित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो संतानों में जनकों के गुणों को बनाए रखती है।
➤ प्रत्येक जीव में ऐसे अनेक गुण होते हैं जो माता-पिता से उसे प्राप्त होते हैं।
➤ ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहते हैं और उन्हीं के आधार पर संतानों की पहचान होती है।
➤ इन विशेषताओं को आनुवंशिक गुण (Heredity Characters) कहते हैं।
➤ आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीवविज्ञान की एक विशेष शाखा आनुवंशिकी (Genetics) में किया जाता है।
➤ किसी जीव की जीनों की समग्र संरचना को उसका जीनप्ररूप (Genotype) कहा जाता है।
➤ जबकि किसी जीव के दिखाई देने वाले गुणों (जैसे – रंग, आकार, ऊँचाई) को प्रकटनप्ररूप (Phenotype) कहा जाता है।
मेंडल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel’s Laws of Inheritance)
ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor Johann Mendel, 1822–1884) को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक (Father of Genetics) कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया कि माता-पिता के गुण किस प्रकार संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं।
➤ मेंडल ने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए Pisum sativum (साधारण मटर के पौधे) का चयन किया, क्योंकि उसमें कई स्पष्ट और आसानी से पहचाने जाने वाले विपरीत गुण (Contrasting Traits) पाए जाते हैं, जैसे – लम्बा/बौना पौधा, पीला/हरा बीज, चिकना/झुर्रीदार बीज आदि।
➤ मेंडल ने अपने प्रयोगों में विपरीत गुणों वाले पौधों को चयनित किया। उदाहरण के लिए: एक लंबे पौधे (Tall plant) और एक बौने पौधे (Dwarf plant) का क्रॉस करवाया।
➤ उन्होंने बौने पौधे के सभी फूलों के पुंकेसर (Stamens) निकाल दिए ताकि स्व-परागण न हो सके, और फिर लंबे पौधे से परागकण लेकर बौने पौधे के वर्तिकाग्र (Stigma) पर गिराए।
➤ इस प्रक्रिया से बने क्रॉस को जनक पीढ़ी (Parental Generation) कहा गया और इन्हें P अक्षर से दर्शाया गया।
F1 पीढ़ी (First Filial Generation – F1)
➤ जब P पीढ़ी के पौधों से परागण के बाद बीज बने और अंकुरित हुए, तो सभी पौधे लंबे (Tall) निकले।
➤ इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा गया और इसे Tt जीनप्ररूप द्वारा दर्शाया गया।
➤ इसमें लंबा गुण (T) प्रभावी (Dominant) था जबकि बौना गुण (t) अप्रभावी (Recessive)।
➤ चूंकि सभी पौधे Tt थे, इसलिए उन्हें संकर (Hybrid) कहा गया क्योंकि उनमें दोनों प्रकार के जीन मौजूद थे।
F2 पीढ़ी (Second Filial Generation – F2)
➤ जब F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में प्रजनन कराया गया (Tt × Tt), तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई।
➤ F2 पीढ़ी में पौधों के बीच निम्नलिखित अनुपात पाया गया:
▪ 3:1 का लक्षणात्मक अनुपात (Phenotypic Ratio) – 3 लंबे : 1 बौना
▪ 1:2:1 का जीनप्ररूपीय अनुपात (Genotypic Ratio) – 1 TT : 2 Tt : 1 tt
➤ इसका अर्थ यह है कि 75% पौधे लंबाई के लक्षण को दर्शाते हैं जबकि 25% पौधे बौने होते हैं।
प्रयोग का निष्कर्ष और मेंडल के नियम
मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के निम्नलिखित तीन मूल नियमों की स्थापना की:
1. पृथक्करण का नियम (Law of Segregation)
➤ यह मेंडल का प्रथम नियम है।
➤ इसके अनुसार, गुणों को नियंत्रित करने वाले दो जीन (एक पिता से और एक माता से प्राप्त) संतान में पृथक-पृथक रहते हैं और किसी एक का प्रभुत्व (Dominance) हो सकता है।
➤ अप्रभावी गुण (Recessive) भी लुप्त नहीं होते, बल्कि F1 पीढ़ी में दबे रहते हैं और F2 में पुनः प्रकट हो सकते हैं।
2. स्वतंत्र संयोजन का नियम (Law of Independent Assortment)
➤ यह नियम मेंडल के द्वि-संकर संकरण (Dihybrid Cross) पर आधारित है।
➤ जब दो या अधिक गुणों का एक साथ अध्ययन किया जाए, तो एक गुण का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; वे स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं।
3. प्रभुत्व का नियम (Law of Dominance)
➤ यह नियम बताता है कि जब दो विभिन्न जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, तो उनमें से एक (प्रभावी) गुण ही प्रकट होता है, जबकि दूसरा (अप्रभावी) दब जाता है।
स्वतंत्र विन्यास का नियम (Mendel’s Law of Independent Assortment) :-
जब दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पौधों को एक साथ क्रॉस किया जाता है, तब हर एक गुण अगली पीढ़ी में अपने-अपने स्वतंत्र रूप से संचारित होते हैं, अर्थात् एक गुण का दूसरे गुण पर कोई प्रभाव नहीं होता।
➤ इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधों में दो विपरीत लक्षणों के जोड़ों का चयन किया और उनके वंशानुक्रम (inheritance) का अध्ययन किया।
➤ इस प्रयोग को द्विगुण संकरण (Dihybrid Cross) कहा जाता है क्योंकि इसमें एक साथ दो लक्षणों (बीज का आकार और रंग) का अध्ययन किया गया।
➤ प्रयोग में एक प्रकार के पौधे के बीज गोलाकार और पीले थे जबकि दूसरे प्रकार के पौधे के बीज झुर्रीदार और हरे रंग के थे।
➤ इन दोनों पौधों के संकरण के बाद प्राप्त सभी F1 पीढ़ी के पौधों में केवल गोलाकार और पीले बीज उत्पन्न हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये दोनों गुण प्रभावी (dominant) हैं।
➤ जब इन F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में कुल चार प्रकार के बीज पाए गए –
- गोल और पीले
- गोल और हरे
- झुर्रीदार और पीले
- झुर्रीदार और हरे
➤ इन बीजों का लक्षण प्ररूपी अनुपात (Phenotypic ratio) 9:3:3:1 पाया गया, जो यह सिद्ध करता है कि बीज का रंग और आकार दो अलग-अलग लक्षण हैं जो संतानों में स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं।
लिंग निर्धारण (Sex Determination) :-
किसी जीव का नर या मादा होना उसके कोशिकाओं में उपस्थित विशेष क्रोमोसोमों के संयोजन पर निर्भर करता है, जिसे लिंग निर्धारण कहते हैं।
➤ प्रत्येक मनुष्य की कोशिकाओं में कुल 23 जोड़े (46) क्रोमोसोम होते हैं।
➤ इनमें से 22 जोड़े सामान्य क्रोमोसोम (Autosomes) कहलाते हैं, जो शरीर की सामान्य विशेषताएं निर्धारित करते हैं।
➤ तेईसवाँ जोड़ा विशेष प्रकार का होता है जिसे लिंग-क्रोमोसोम (Sex Chromosomes) कहा जाता है।
➤ लिंग-क्रोमोसोम दो प्रकार के हो सकते हैं – X और Y।
▪ मादा (Female) के पास दो समान लिंग-क्रोमोसोम होते हैं – XX।
▪ नर (Male) के पास दो भिन्न लिंग-क्रोमोसोम होते हैं – XY।
➤ जब निषेचन (fertilization) होता है:
▪ यदि X शुक्राणु अंडाणु से मिल जाए, तो संतान मादा (XX) होगी।
▪ यदि Y शुक्राणु अंडाणु से मिल जाए, तो संतान नर (XY) होगी।
➤ यह सिद्धांत दर्शाता है कि लिंग निर्धारण में पुरुष का योगदान निर्णायक होता है, क्योंकि वही X या Y कोई भी प्रकार का शुक्राणु प्रदान कर सकता है।
➤ इस पूरी प्रक्रिया को हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत (Theory of Heterogamety) कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि नर दो प्रकार के युग्मक (X और Y) उत्पन्न करता है जबकि मादा केवल एक ही प्रकार के (X) युग्मक बनाती है।
जैव विकास (Organic Evolution) :-
प्रकृति में जीवन का प्रारंभ बहुत ही सरल जीवों से हुआ, लेकिन समय के साथ बदलते पर्यावरण और परिस्थितियों के प्रभाव से इन सरल जीवों में धीरे-धीरे कई परिवर्तन होते गए।
➤ इन्हीं परिवर्तनों के चलते आज पृथ्वी पर जटिल और विविध प्रकार के जीवों की उपस्थिति देखी जाती है।
➤ सजीवों में समय के साथ होने वाले इन स्थायी और उत्तराधिकार में जाने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं।
➤ यह विकास धीरे-धीरे लाखों वर्षों में हुआ और यह दर्शाता है कि सभी जीव किसी-न-किसी प्रारंभिक रूप से उत्पन्न हुए हैं और परस्पर संबंधित हैं।
उपार्जित लक्षण (Acquired Characters) :-
जंतु के शरीर में ऐसे परिवर्तन जो वातावरण के प्रभाव, जीवन शैली या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है।
➤ ये परिवर्तन जीवनकाल के दौरान होते हैं और पहले ऐसा माना जाता था कि ये अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो सकते हैं।
➤ इस सिद्धांत को सबसे पहले लामार्क (Lamarck) ने प्रस्तुत किया था, जिसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत (Theory of Inheritance of Acquired Characters) कहा जाता है।
➤ लामार्क ने 1809 में अपने विचारों को Philosophie Zoologique नामक पुस्तक में प्रकाशित किया।
➤ उदाहरण के लिए: जिराफ़ की लम्बी गर्दन – लामार्क के अनुसार जिराफ़ पेड़ की ऊँचाई तक पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन खींचता रहा जिससे वह लम्बी हो गई और यह गुण संतानों में स्थानांतरित हुआ।
आनुवांशिक लक्षण (Genetic Characters) :-
जंतु या पौधे में ऐसे लक्षण जो उसे जन्म से ही माता-पिता से प्राप्त होते हैं, वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं।
➤ ये लक्षण जीन के माध्यम से जनन कोशिकाओं (Gametes) में होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं।
➤ आनुवंशिक लक्षण स्थायी होते हैं और जैव विकास की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
➤ ये लक्षण संतान के बाहरी स्वरूप (Phenotype) और जीन संरचना (Genotype) दोनों को प्रभावित करते हैं।
➤ उदाहरण: मनुष्य के आँखों का रंग, बालों की बनावट, त्वचा की रंगत आदि।
जाति उद्भवन (Speciation) :-
जब किसी एक ही जाति के जीवों के बीच प्रजनन की क्षमता किसी कारणवश बाधित हो जाती है और वे दो अलग-अलग समूहों में बँट जाते हैं, जो आगे चलकर अलग-अलग जातियों के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को जाति उद्भवन कहते हैं।
➤ यह प्रक्रिया तब होती है जब किसी जीव समूह में जननिक परिवर्तन (Genetic change) और प्रजनन अवरोध (Reproductive isolation) उत्पन्न हो जाए।
➤ इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं –
(1) विस्थानिक जाति उद्भवन (Allopatric Speciation)
(2) समस्थानिक जाति उद्भवन (Sympatric Speciation)
(1) विस्थानिक जाति उद्भवन (Allopatric Speciation) :-
जब एक जाति की कुछ जनसंख्या भौगोलिक रूप से शेष जनसंख्या से अलग हो जाती है – जैसे पहाड़, नदी, रेगिस्तान आदि के कारण – तो लंबे समय के बाद इनमें जननिक परिवर्तन हो जाते हैं।
➤ यह परिवर्तन दोनों जनसंख्याओं को इतना अलग बना देता है कि वे दोबारा संपर्क में आने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते।
➤ इस स्थिति में वे दो अलग-अलग जातियाँ बन जाती हैं।
➤ यह पृथक्करण धीरे-धीरे हजारों वर्षों में होता है और इसका कारण प्राकृतिक बाधाएँ होती हैं।
(2) समस्थानिक जाति उद्भवन (Sympatric Speciation) :-
जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक जाति की जनसंख्या जननिक परिवर्तन या व्यवहारिक, पोषणीय या अन्य कारणों से एक-दूसरे से अलग हो जाती है और उनमें प्रजनन अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वे धीरे-धीरे दो अलग जातियों में विकसित हो जाती हैं।
➤ इसमें भौगोलिक बाधा नहीं होती, बल्कि आंतरिक कारणों से वे एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं।
➤ यह प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम सामान्य होती है लेकिन जीन स्तर पर भिन्नता इसके मूल में होती है।
समजात अंग (Homologous Organs) :-
ऐसे अंग, जो संरचना तथा उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक जैसे होते हैं, लेकिन वे अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं।
➤ उदाहरण: मनुष्य का हाथ, पक्षियों का पंख, व्हेल की पंख और घोड़े का अगला पैर — इन सभी की आंतरिक बनावट समान होती है, पर ये अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे पकड़ना, उड़ना, तैरना, दौड़ना आदि।
➤ यह दर्शाता है कि इन अंगों का एक समान पूर्वज रहा है और ये विकास की समान दिशा (divergent evolution) के प्रमाण हैं।
असमजात अंग (Analogous Organs) :-
ऐसे अंग, जो एक जैसे कार्य करते हैं लेकिन उनकी संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है, असमजात अंग कहलाते हैं।
➤ उदाहरण: पक्षियों के पंख और कीड़ों के पंख — दोनों उड़ने के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन उनकी बनावट तथा विकासक्रम अलग-अलग होता है।
➤ यह समरूपी विकास (convergent evolution) का उदाहरण है, जहाँ अलग-अलग जीवों में समान कार्यों के लिए अंग विकसित होते हैं।
जीवाश्म (Fossil) :-
भूतकाल में पृथ्वी पर पाए गए ऐसे जीव जो अब विलुप्त हो चुके हैं, उनके शरीर के अवशेष या उनके द्वारा छोड़े गए चिन्ह जो चट्टानों में दबे मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं।
➤ जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन जीव कैसे थे और वे वर्तमान जीवों से कैसे भिन्न या समान थे।
➤ जीवाश्मों का अध्ययन “जीवाश्मविज्ञान” (Palaeontology) कहलाता है।
➤ जीवाश्म की आयु जानने के दो प्रमुख तरीके हैं –
(i) जिस गहराई से जीवाश्म प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर अनुमान।
(ii) रेडियोकार्बन काल-निर्धारण (Radiocarbon Dating) विधि द्वारा सटीक आयु ज्ञात की जाती है।
आणविक जातिवृत (Molecular Phylogeny) :-
किसी जीव के DNA अनुक्रमों की तुलना करके उसके पूर्वजों का पता लगाने की प्रक्रिया को आणविक जातिवृत कहते हैं।
➤ इसमें विभिन्न जीवों के DNA और RNA की बनावट का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन-कौन से जीव एक-दूसरे से अधिक निकट संबंध रखते हैं।
➤ यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो जैव विकास को आणविक स्तर पर प्रमाणित करती है।
निष्कर्ष (Conclusion):
अगर आपको यह कक्षा 10वीं जीव विज्ञान – अध्याय: अनुवांशिकता एवं जैव विकास (Genetics and Evolution) के नोट्स उपयोगी लगे हों, तो ऐसे ही सरल, संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studynumberone.Co को जरूर विज़िट और फॉलो करें।
यहाँ आपको कक्षा 10 के सभी विषयों — जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, एवं सामाजिक विज्ञान आदि के नवीनतम और बोर्ड परीक्षा आधारित नोट्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं।
More Notes